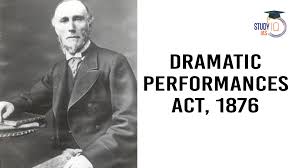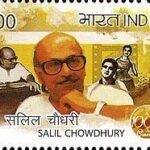(इप्टा के दस्तावेज़ीकरण के अन्तर्गत रमेशचन्द्र पाटकर द्वारा मराठी में लिखी एवं संपादित की हुई किताब ‘इप्टा : एक सांस्कृतिक चळवळ (इप्टा : एक सांस्कृतिक आंदोलन) के चौथे हिस्से में ‘परिशिष्ट’ में चार प्रकार के महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ संकलित हैं। इसमें से तीन परिशिष्ट मुंबई इप्टा की गतिविधियों से संबंधित हैं। पहला परिशिष्ट इस मायने में बहुत महत्त्वपूर्ण है कि, जिस काले ब्रिटिश क़ानून की अनेक सांस्कृतिक दस्तावेज़ों में चर्चा की जाती है, उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है। यह लेख प्रमिला पंधे संपादित अंग्रेज़ी किताब ‘Suppression of Drama in Nineteenth Century India’ के कुछ अंशों को उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए रमेशचन्द्र पाटकर ने मराठी में अनूदित कर संकलित किया गया है।
यह दस्तावेज़ इस मायने में भी महत्त्वपूर्ण है कि आज से लगभग डेढ़ सौ साल पहले क़ानून-व्यवस्था का अंग्रेजों का जो मॉडेल था, आज के शासन-प्रशासन द्वारा उसका अनुकरण और भी अद्यतन तरीक़ों से किया जा रहा है।
सभी फोटो गूगल से साभार।)
स्वतंत्रता के लिए 1857 का विद्रोह ब्रिटिशों द्वारा कुचल दिया गया था। उसके बाद देश की मेहनतकश जनता के हर प्रकार के दमन के लिए सरकार ने अपना जाल फैलाया। तत्कालीन भारतीय लेखकों ने ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जनता के रोंगटे खड़े करने वाले क्रूर शोषण की परिस्थितियों का चित्रण किया था।

नील की फसल लेने वाले किसानों के जीवन की भीषण परिस्थितियों का चित्रण बांग्ला में ‘नील दर्पण’ नाटक में किया गया था। यह नाटक 1861 में प्रकाशित हुआ। ‘द इंग्लिशमैन’ नामक अंग्रेज़ी तथा ‘हुरकाल’ नामक बांग्ला अख़बार में इसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध की आवाज़ें उठीं। अंग्रेज़ लेखक रेवरंड जेम्स लाँग ने इस नाटक का अंग्रेज़ी अनुवाद किया था।
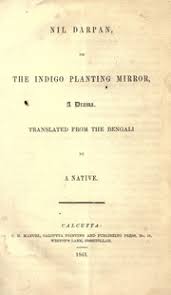
अन्य फसलें उगाने वाले तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सब कुछ सहन करने वाले बंगाल के किसानों को नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश कंपनियाँ ज़ोर-ज़बर्दस्ती कर रही थीं और उन्हें यातना दे रही थीं। वे जिन पारंपरिक फसलों को उगाते थे, उनके स्थान पर नील की फसल लगाने के लिए सख़्ती की जा रही थी, जिससे ज़मीन अनुपयोगी होकर किसानों को ग़ुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था। इस नाटक में इसका चित्रण प्रभावी तरीक़े से सीधी-सादी भाषा में किया गया था। “ब्रिटिश बाग़ान-मालिकों के पक्ष में दिये गये निर्णय तथा पिछले साल नील के ठेकेदारों को कठोर दंड देने संबंधी क़ानून का संदर्भ” इस नाटक में दिया गया है, रेवरंड जेम्स लाँग ने अपने अंग्रेज़ी अनुवाद की प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया है।


भारत के ब्रिटिश ज़मींदारों के संगठन ने इस नाटक के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई। रेवरंड जेम्स लाँग पर मुक़दमा ठोंक दिया गया। न्यायालय ने उसे एक महीने की सज़ा और एक हज़ार रुपये का दंड घोषित किया। इस पर रेवरंड जेम्स लाँग ने कहा, “माय लॉर्ड, न्यायालय ने नाटक को दंडनीय कहा है, इसलिए उसके द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करना और तदनुसार व्यवहार करना मैं अपना फ़र्ज़ मानता हूँ। मगर ज्यूरी द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार मैंने किसी प्रकार का अनैतिक व्यवहार या अपराध नहीं किया है। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ यही कहती है।”

रेवरंड जेम्स लाँग को सज़ा होने के बावजूद देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करने वाले और भी नाटक बंगाल में लगातार लिखे जाने लगे। रेवरंड जेम्स लाँग पर लगाए गए जुर्माने की रक़म का भुगतान एक ‘लोकहितवादी’ भारतीय ने किया। नाटक के शीर्षक का शब्द ‘दर्पण’ लोकप्रिय हो गया।
ब्रिटिश जहाज़-मालिकों द्वारा ख़लासियों के किए जाने वाले शोषण पर आधारित ‘समुद्र दर्पण’; एक ब्रिटिश अधिकारी को ज़हर खिलाने का झूठा आरोप बड़ौदा के महाराज पर थोपकर एक ‘षड़यंत्र रचने’ संबंधी मुक़दमा सरकार ने दायर किया। ब्रिटिश शासन उनसे बदले की भावना का व्यवहार करता था। इसका चित्रण करने वाला ‘गायेकवार दर्पण’ तथा दक्षिणचरण चट्टोपाध्याय द्वारा असम के चाय-बाग़ानों के मज़दूरों के शोषण को दर्शाने वाला नाटक ‘चाकार दर्पण’ उन दिनों ब्रिटिश शासन के क्रोध का शिकार हुए। ये सभी नाटक जनता में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। भारत के ब्रिटिश पूँजीपति तथा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण नाट्य-लेखन का विषय बन गए थे। ये नाटक शोषण के विरोध में दर्शकों के मन में ग़ुस्से की लहर पैदा करते थे और उनमें देश-भक्ति की भावना जगाते थे।

‘गायेकवार दर्पण’ नाटक के मंचन करने वाली ‘द ग्रेट नेशनल थिएटर कंपनी’ के विरुद्ध ब्रिटिश शासन द्वारा कड़े कदम उठाए गए। कुछ युवा कलाकारों को गिरफ़्तार किया गया। अगर किसी व्यक्ति की भावनाएँ आहत होती हों और उसके द्वारा कोई शिकायत दर्ज़ की जाती हो तो ‘भारतीय दंड संहिता’ (Indian Penal Code) के अनुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है। मगर कार्रवाई करने में अक्सर देर हो जाती थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार को तीव्रता से महसूस हुआ कि इस तरह के देशभक्तिपरक नाटकों पर पाबंदी लगाने के लिए और कठोर अधिकारों का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। हालाँकि क़ानून की परवाह किए बिना ग्रामीण और अन्य भागों के पुलिस अधिकारी इन नाटकों पर तुरंत कार्रवाई करते थे, मगर कलकत्ते में उन्हें यह करना मुश्किल होता था।
‘हिंदू हितैषी’ नामक अख़बार के 22 अप्रैल 1876 के अंक में इन परिस्थितियों के प्रत्यक्ष अनुभव पर भाष्य प्रकाशित किया गया था। ‘चाकार दर्पण’ नामक नाटक में चाय-बाग़ान में काम करने वाले मज़दूरों की अवस्था का चित्रण किए जाने पर एंग्लो-इण्डियन समाज इस नाटक से बेहद ख़फ़ा हो गया और उसके बाद प्रशासन द्वारा उनकी निरंतर प्रताड़ना की जाने लगी। शायद इसके कारण ही ब्रिटिश शासन को ‘नाट्य-प्रस्तुतियों पर प्रतिबंध’ संबंधी क़ानून मंज़ूर करने का अवसर मिल गया।

भारत में ब्रिटिशों की दुराचारी राजसत्ता के विरुद्ध भारतीय जनता में बड़े पैमाने पर पैदा होने वाला असंतोष और अंकुरित होने वाली देशभक्ति की भावना को हमेशा के लिए कुचलने के लिए विधानसभा में लाए गए इस विधेयक पर राज्य-शासन में काफ़ी बहस-मुबाहिसा हुआ। मगर इस विधेयक को मंज़ूर करवाने के लिए ब्रिटिश सत्ता ने ज़मीन-आसमान एक कर दिया। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लिखे गए साहित्य के अलावा किसी नाटक में किसी ब्रिटिश अधिकारी पर कोई अप्रत्यक्ष टिप्पणी दिखाई देती थी तो उसके लिए भी इस विधेयक में सज़ा का प्रावधान था। यह विधेयक आगे चलकर क़ानून में रूपांतरित हो गया। इसे ‘1876 के नाट्य-प्रस्तुति प्रतिबंधक क़ानून’ के नाम से जाना जाता है। (डेढ़ सौ वर्षों बाद भी परिस्थिति में कितना साम्य है!!)अश्लील तथा घृणास्पद चित्रण किए जाने वाले नाटकों पर भी प्रतिबंध लगाने की सुविधाजनक तथा चालबाज़ व्यवस्था इस क़ानून में की गई थी।
समकालीन अख़बारों में छपी हुई प्रतिक्रियाएँ :
नाट्य-प्रस्तुति प्रतिबंधक विधेयक और क़ानून पर तत्कालीन अख़बारों में कुछ प्रतिक्रियाएँ प्रकाशित की गई थीं।
‘अमृत बाज़ार पत्रिका’ बंगाल का अत्यंत प्रतिष्ठित समाचारपत्र है। इसके 25 दिसंबर 1874 के अंक में प्रकाशित अग्रलेख ‘कौन अधिक शुभचिंतक : पुलिस या बाग़ान-मज़दूर?’ का सारांश इस प्रकार है : नील की खेती करने वाले किसानों तथा ब्रिटिशों के बाग़ानों में काम करने वाले मज़दूरों के संदर्भ में ‘ज़मींदार संगठन’ द्वारा न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त अग्रलेख में अपील की गई थी कि किसानों और मज़दूरों को काम से न हटाया जाए। इस लेख में अनेक घटनाओं का ज़िक्र किया गया था कि जिसमें अमीरों का पक्ष-पोषण ही किया गया तथा ग़रीबों को तवज्जो नहीं दी गई थी। बल्कि उन्हें दमन का सामना करने के लिए बाध्य किया गया। नील की खेती करने वाले किसानों ने अपने ऊपर पर्याप्त नियंत्रण रखा है, परंतु जब उन्हें उनके खेतों से खदेड़ दिया जाता है तब उनकी मदद करने की बजाय पुलिस उन्हें ही परेशान करती है। अगर पुलिस पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो उन्हें ही इसका फ़ायदा होगा और अगर नियंत्रण में रखा गया तो उन्हें नुक़सान का सामना करना पड़ेगा। … पुलिस जनता के संपर्क में होती है। इसकी तुलना में किसान और बाग़ान-मज़दूरों का संबंध लोगों से काफ़ी कम होता है। किसान और मज़दूर डर और आतंक के दबाव में काम करते हैं, मगर पुलिस निडर होकर घूमते हैं। बाग़ान-मज़दूरों का होने वाला शोषण देश के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। मज़दूरों को दी जाने वाली यातनाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है, मगर पुलिस के मामले में यह नहीं कहा जा सकता। मज़दूरों का मुँह बंद किया जा सकता है, मगर पुलिस को देश के सम्मान और प्रतिष्ठा का रखवाला कहा जाता है। शक्तिशाली सरकार और दंडाधिकारियों के वे सेवक होते हैं। अपनी रोज़ी-रोटी सुरक्षित रखने के लिए वे मज़दूर और किसानों पर ज़ोर-ज़बरदस्ती कर सकते हैं। पुलिस वर्चस्व में हम अपना आत्मसम्मान, धीरज और विश्वास खोते जा रहे हैं। हम कमज़ोर और कायर हो गए हैं। हिंदू और मुस्लिमों वंशों की राष्ट्रीय जीवनी-शक्ति कुचल दी गई है तथा ब्रिटिश शासन द्वारा हमारी प्रगति और विकास के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा किया गया है। पुलिस के अधिकारों को नियंत्रित करना देश के लिए लाभकारी होगा। उनके अधिकारों में वृद्धि करने पर वे निश्चित रूप से देश को बर्बाद कर देंगे; इसीलिए पुलिस के अधिकारों को तत्काल सीमित किया जाना चाहिए। इस तरह के कुछ उपायों को लागू करने पर दर्ज़ किए गए झूठे मुक़दमों से जनता की रक्षा हो पाएगी तथा निर्दोष लोगों को जेल जाने से बचाया जा सकेगा। अपने उच्चाधिकारियों को खुश करने के लिए पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है।

‘सोम प्रोकाश’ नामक बांग्ला अख़बार ने 25 जनवरी 1874 के अंक में इस क़ानून पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसमें कहा गया था कि जिन ज़िलों में चाय-बाग़ान हैं, वहाँ के बाग़ान-मालिक अपने मज़दूरों पर निरंतर अत्याचार करते हैं। इसके बावजूद अक्सर मुक़दमों का फ़ैसला मालिकों के पक्ष में ही आता है। इस अख़बार में ठेका पद्धति की आलोचना करते हुए कहा गया है कि इन ज़िलों में जब तक ठेके पर मज़दूर रखने की पद्धति अपनाई जा रही है, तब तक तानाशाही चलती रहेगी। इसलिए ठेका पद्धति को समाप्त करते हुए चाय-बाग़ानों में मज़दूरों से स्वतंत्र रूप से काम करवाया जाए। मज़दूरों को क़ानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इसके लिए राज्य में कई न्यायालय खोलने पड़ेंगे।
‘संसद प्रभाकर’ नामक बांग्ला अख़बार के 01 जुलाई 1875 के अंक में ‘चाकार दर्पण’ के अंग्रेज़ी अनुवाद का संदर्भ देते हुए संवाददाता ने लिखा है कि ‘चाकार दर्पण’ में बाग़ानों के मज़दूरों पर किए जाने वाले अत्याचारों का जो चित्रण किया गया है, उससे कई गुना ज़्यादा अत्याचार प्रत्यक्ष में किए जाते हैं। चाय-बाग़ान के मालिकों में अपवादस्वरूप कुछ भले लोग भी हैं, मगर अधिकांश बाग़ान-मालिक अत्याचारी ही हैं। असम में तो ख़ुद सरकार ही एक पैसा दिए बिना काम करने के लिए मज़दूरों पर ज़बर्दस्ती करती है। मज़दूरों को मजबूर होकर काम करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

बंगाल की तरह ही मुंबई के कुछ अख़बारों ने इस नाट्य-प्रस्तुति प्रतिबंधक क़ानून पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है। ‘द बॉम्बे समाचार’ नामक गुजराती अख़बार ने 04 मार्च 1876 के अंक में लिखा कि यह क़ानून बनाकर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एकतरफ़ा हमला किया है। नैतिक मूल्यों के बारे में प्रतिकूल राय रखने वाले या किसी व्यक्ति का चरित्र-हनन करने वाली नाट्य-प्रस्तुतियों पर पाबंदी लगाना उचित हो सकता है, फिर भी राजनीतिक घटनाओं पर उचित तरीक़े से व्यक्त की जाने वाली भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने के किए क़ानून बनाने की जो मुस्तैदी दिखाई गई है और जिस तरह की चिंता दर्शाई गई है, उससे यह साबित होता है कि ब्रिटिशों को देश के अख़बारों से कितना डर लग रहा है! इसीलिए इस स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। समाज के प्रसिद्ध व्यक्तियों की बदनामी करने वाले नाटक को नाटक न कहा जाए। इस तरह के नाटक दर्शकों को भ्रमित करते हैं, अतः इस तरह के नाटकों का ‘बंदोबस्त’ किया जाए, यह बात ‘अखबारे सौदागर’ नामक अख़बार के 11 मार्च 1875 के अंक में प्रकाशित की गई थी।
‘अरुणोदय’ नामक अंग्रेज़ी-मराठी अख़बार में 09 अप्रैल 1875 को एक लेख प्रकाशित किया गया, जिसमें लार्ड नॉर्थब्रुक के पुतले की स्थापना के संदर्भ में नाट्य-प्रस्तुति प्रतिबंधक क़ानून की आलोचना की गई, जो इस प्रकार है :
“प्रस्तुत क़ानून कितना संदेहास्पद है और उसमें बचाव के कितने प्रकार के चोर-रास्ते रखे गए हैं, इस बात की पड़ताल करते हुए लेखक कहता है कि क़ानून में प्रावधान किया जा रहा है कि, जब कोई नाटक वीभत्स तथा प्रतिष्ठा-हनन का प्रयास करने वाला हो तो उस नाटक के मंचन पर दंडाधिकारी द्वारा तत्काल पाबंदी लगानी चाहिए तथा इसे अंतिम निर्णय मानना चाहिए। दंडाधिकारी को प्रदत्त किया गया यह अधिकार मनमाना निर्णय लेने की पूरी छूट प्रदान करता है। हालाँकि इसके लिए वर्तमान में विद्यमान क़ानून में ही उचित प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति को महसूस होता है कि किसी नाट्य-प्रस्तुति से उसकी बदनामी होती है, तो उसे या उस जैसे अन्य लोगों को भी दीवानी या फ़ौजदारी न्यायालय में जाना चाहिए। इस तरह के प्रकरण में सरकारी अधिकारियों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए?” ( कुछ दिनों पहले घटी कुछ घटनाओं से इसका कितना साम्य है!!)
‘ज्ञानप्रकाश’ नामक अंग्रेज़ी-मराठी अख़बार में ‘नाट्य-प्रस्तुति प्रतिबंधक विधेयक’ शीर्षक का लेख मोटे अक्षरों में 17 अप्रैल 1875 को प्रकाशित हुआ था। इस लेख में लिखा गया था : “जनता की वास्तविक आवश्यकताएँ क्या हैं? और इनकी पूर्ति करने के क्या उपाय हो सकते हैं? इसकी कोई चर्चा न करते हुए सरकार सिर्फ़ क़ानूनों का पालन करती रहती है। किए जाने वाले उपायों से जनता के हित किस तरह बाधित होते हैं, इस बाबत विचार न करते हुए, इसके बारे में जनता का मत जानने के लिए पर्याप्त समय न देते हुए सरकार जल्द से जल्द क़ानून को लागू करना चाहती है। इसके कारण जनता के मन में असुरक्षा तथा अविश्वास की भावना पैदा होती है।
जनता को दुखाना या उसमें असुरक्षा पैदा करना शायद सरकार का उद्देश्य न भी हो, परंतु सरकार के विश्वसनीय अधिकारी ग़लत उद्देश्य से या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह के हानिकारक क़ानूनों का सहारा लेते हैं। तत्कालीन सर्वोच्च विधान-मण्डल के पटल पर रखा जाने वाला ‘नाट्य-प्रस्तुति प्रतिबंधक विधेयक’ इसका उदाहरण है। अपने विधेयक के समर्थन में माननीय मि. हॉब हाउस ने प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुँचाने वाले तथा अपमान करने वाले नाटकों का उल्लेख किया है। हालाँकि इस प्रकार के क़ानून की आवश्यकता न होने की बात ख़ुद सदस्य महोदय द्वारा अपनी दलील में कही गई है। ‘ज्ञानप्रकाश’ ने इस बात को भी रेखांकित किया था।
कुछ वर्ष पहले प्रकाशित हुई एक जीवनी के कारण मुंबई में दहशत पैदा करने वाला एक दंगा हुआ था। बावजूद इसके, अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने वाला क़ानून तैयार करने के लिए यह ठोस कारण नहीं माना जा सकता। सारांश में, मानहानि का मुक़दमा दायर करने योग्य व्यक्तियों को इस कष्ट से बचाने के लिए एक नया क़ानून बनाए जाने की आवश्यकता कदापि नहीं है।
नाट्य-प्रस्तुति प्रतिबंधक क़ानून के बारे में उस समय जनता में बहुत उत्सुकता पैदा हुई थी, इसकी झलक तत्कालीन अख़बारों में छपे उपर्युक्त लेखों और रिपोर्टों से मिल सकती है। जनता का तथा लेखक-कलाकारों की रचनात्मक स्वतंत्रता का हनन करने वाली ब्रिटिश राजसत्ता के विरोध में किस तरह जनमत जागृत हो रहा था, उपर्युक्त उद्धरण यह दर्शाते हैं।