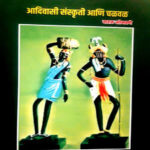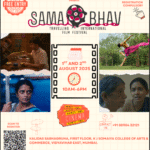- एडवोकेट निशा शिवूरकर
- हिन्दी अनुवाद – उषा वैरागकर आठले
कनाडा में 06 दिसम्बर 1989 को स्त्रीवाद के प्रति विरोध और स्त्रियों के प्रति नफ़रत के कारण माँट्रियल हत्याकाण्ड घटित हुआ। इस बात का अहसास होने पर पुरुषों ने ही पहल करते हुए पुरुषसत्तात्मक मानसिकता को बदलने का बीड़ा उठाया। इसके फलस्वरूप दुनिया भर में ‘मेन फॉर चेंज’, ‘मेन कैन स्टॉप रेप’, ‘प्रो फेमिनिस्ट मेन्स ग्रुप’, ‘मेनली मेन अगेंस्ट वॉयलेंस एण्ड सेक्सिज़्म’ जैसे पुरुषों के संगठन गठित हुए। हमारे देश में इसके पहले से ही कुछ संतों और समाज-सुधारक पुरुषों द्वारा स्त्री के प्रति आदर व्यक्त किया जाता रहा है। उनके द्वारा किए गए कार्य स्त्री-आंदोलन को बल प्रदान करते रहे हैं।
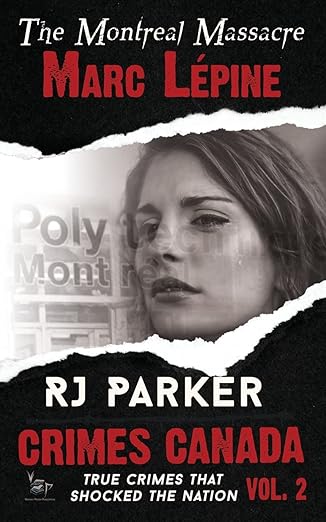
कनाडा के माँट्रियल शहर में घटी एक भयानक घटना पर दुनिया भर के माध्यमों का ध्यान गया था। यह घटना 06 दिसम्बर 1989 को ‘इकोल पॉलीटेक्निक कॉलेज’ की एक कक्षा में दोपहर को घटित हुई थी। मार्क लिपाइन नामक 25 वर्षीय एक युवक हाथों में बंदूक़ और चाकू लेकर अचानक कक्षा में घुसा और उसने कक्षा के तमाम छात्रों को बाहर निकलने का आदेश देकर छात्राओं पर ताबड़तोड़ गोलियाँ दागीं। अपनी जान बचाने के लिए चीखने-चिल्लाने वाली 14 लड़कियों की लाशें कक्षा में बिछ गईं और अन्य 14 लड़कियाँ गंभीर रूप से घायल हो गईं। बाद में मार्क ने आत्महत्या कर ली। अपने ‘सुसाइड नोट’ में उसने लिखा था, “स्त्रीवादियों के प्रति मेरे मन में बहुत ज़्यादा असंतोष और आक्रोश है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली स्त्रीवादियों को मैंने उनके सृष्टिकर्ता के पास यमलोक भेज दिया है।” मार्क के इस वक्तव्य से स्त्रीवादी संगठनों में हलचल मच गई थी।
दुनिया भर के स्त्रीवादी संगठनों ने इस भयानक हत्याकाण्ड के प्रति निषेध व्यक्त किया। अनेक माध्यमों में अपराधी की स्त्री-द्वेषी प्रवृत्ति के विकास पर शोधपरक लेख प्रकाशित हुए। कनाडा के सामाजिक वातावरण पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा था। घटना के बाद सरकार द्वारा शस्त्रों के प्रयोग संबंधी नियम अधिक कठोर किए गए। कनाडा में 06 दिसम्बर ‘स्त्रियों पर हिंसाचार विरोधी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
माँट्रियल शहर के संवेदनशील और विचारशील पुरुषों को भी इस घटना ने आंदोलित किया था और समविचारी ‘स्त्रीवाद’ समर्थक पुरुषों ने इकट्ठा होकर ‘मेन फॉर चेंज’ नामक संगठन की स्थापना की। यह एक नई शुरुआत थी। संगठन ने इस तरह के हिंसाचार का निषेध करते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट की कि, ‘माँट्रियल हत्याकाण्ड हमारे समाज की स्त्रियों के विरुद्ध की गई करतूत है। यह किसी सिरफिरे का काम नहीं है। जिस मानसिकता के कारण इन लड़कियों की हत्या की गई है, उस हिंसक संस्कृति की जकड़ से स्त्री-पुरुष और बच्चों को मुक्त करने के लिए संगठन के सदस्य प्रतिबद्धता ज़ाहिर करते हैं।”
बहुसंख्यक पुरुष हिंसक नहीं होते। हमारे समाज और परिवार में जिस तरह पुरुषों का लालन-पालन किया जाता है, उससे उनमें आक्रामकता, हिंसा के प्रति आकर्षण पैदा होता है। नर्मदिल आचरण को ‘जनाना’ करार दिया जाता है। ‘मर्दानगी’ की अवधारणा शारीरिक शक्ति के साथ जोड़ दी जाती है। पुरुष का विकास और समाजीकरण इस तरह होता है कि कुछ पुरुष ख़ुद से कमज़ोर स्त्री-पुरुष और बच्चों से बहुत क्रूर और हिंसक व्यवहार करते हैं। इसमें ही वे अपने ‘पुरुषार्थ’ या ‘मर्दानगी’ को महसूस करते हैं। इस तरह के पुरुष स्त्रियों के नकार को, उनके सवालों को बिलकुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। भेदभाव का माहौल और नफ़रत हिंसा को प्रोत्साहित करती है। ‘मेन फॉर चेंज’ संगठन ने पुरुषों के लिए एक आचार-संहिता घोषित की थी, जिसमें कहा गया कि, ‘एक पुरुष के रूप में मुझे जो अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनके तहत मैं किसी पर भी आक्रमण कर सकता हूँ’, इस कल्पना से पुरुषों को मुक्त होना ज़रूरी है। पुरुषों को अपनी भावनाएँ, अपने डरों को खुलकर व्यक्त करना चाहिए। पुरुष मदद कर सकता है, वैसे ही मदद माँग भी सकता है। उन्हें लैंगिक भाषा और शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। स्त्रियों को अपमानित करने वाले विज्ञापनों, माध्यमों का बहिष्कार करना चाहिए, स्त्रियों पर होने वाली हिंसा का विरोध करना चाहिए। उन्हें समाज द्वारा लादी गई तथाकथित पुरुषोचित अपेक्षाओं को नकार देना चाहिए। किसी पर भी सत्ता या कब्ज़ा जमाने की बजाय अपनी क्षमता को साबित किया जा सकता है, इस बात पर विश्वास करना चाहिए। एक पुरुष के रूप में अपने कर्मों की ज़िम्मेदारी ख़ुद लेनी चाहिए। इस तरह की अनेक बातों का समावेश इस आचार-संहिता में किया गया था। संगठन द्वारा स्कूल-कॉलेज में जाकर इस आचार-संहिता को मान्यता दिलाने का आंदोलन छेड़ा गया था।
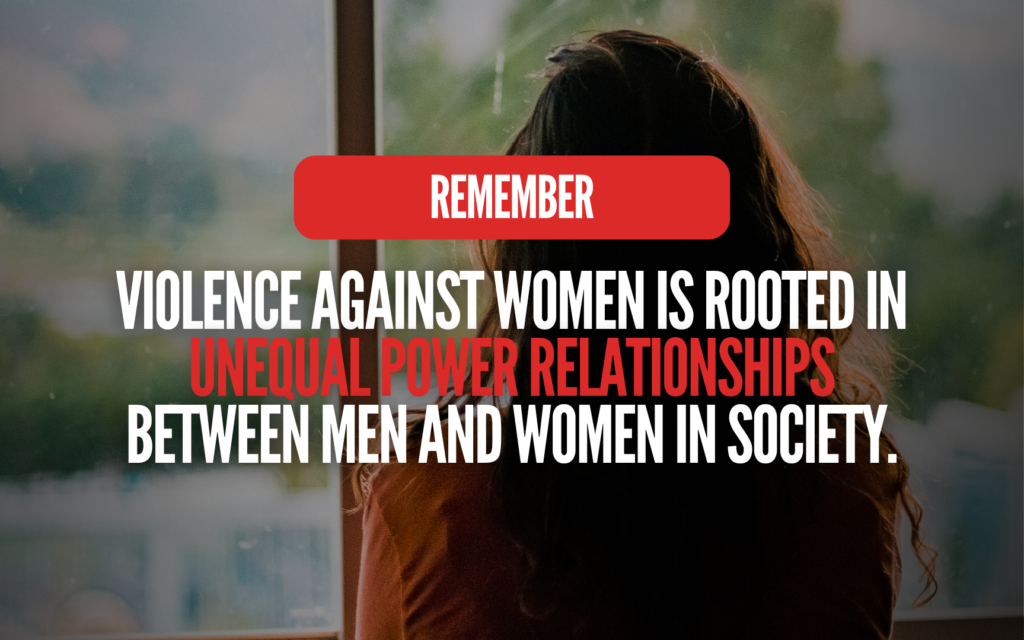
‘मेन फॉर चेंज’ से प्रेरणा लेकर कनाडा में ही ‘मेन कैन स्टॉप रेप’ और ‘प्रो फेमिनिस्ट मेन्स ग्रुप’ जैसे अन्य संगठन भी स्त्री-मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए गठित हुए। आगे चलकर अमेरिका और कनाडा के पुरुषों के एक संयुक्त संगठन ‘मेनली मेन अगेन्स्ट वॉयलेंस एंड सेक्सिज़्म’ (एमएमएवीएस) की स्थापना हुई। संगठन ने अपनी भूमिका में कहा, “पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर की जाने वाली हिंसा अपराध है। स्त्रीविरोधी होने वाले अपराधों को सिर्फ़ स्त्रियों के प्रश्न के रूप में क्यों देखा जाता है? पुरुषों को स्वीकार करना होगा कि हम अपराध करने वाले हैं, अपराध करने वालों के वंशज या मित्र हैं। इसलिए इन अपराधों को रोकने का काम भी पुरुषों का ही है। अगर दुनिया में हिंसा का अंत करना है तो हरेक पुरुष को इसकी शुरुआत ख़ुद से करनी होगी।” पुरुष को एक परिपक्व पुरुष एवं मनुष्य बनने के लिए बदलना होगा। ‘एमएमएवीएस’ ने इस विचार का बीजारोपण किया कि, स्त्रियों के साथ सत्ता और ताक़त साझा करने का विचार क़बूल करने से ही हमारा सच्चा विकास होगा और हम ज़्यादा इंसानियत के साथ जीना सीखेंगे। दुनिया भर के अनेक पुरुष इस संगठन के सदस्य बने।
1991 में इंग्लैंड और वेल्स में स्त्रीवाद-समर्थक पुरुषों द्वारा शुरू की गई ‘व्हाइट रिबन’ संस्था का अनेक देशों में विस्तार हुआ। व्हाइट रिबन द्वारा 25 नवम्बर को स्त्री-हिंसाचार उन्मूलन दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से विशेष आग्रह किया गया। 2010 में इंग्लैंड के प्रेस्टन शहर में गठित किए गए संगठन ‘मेन अगेंस्ट वॉयलेंस’ ने स्त्रियों और बच्चियों पर होने वाले घरेलू और लैंगिक अत्याचार के विरोध में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। ब्रिटिश स्कूलों के पाठ्यक्रम में लैंगिक और घरेलू हिंसाविरोधी शिक्षा लागू करने की माँग की गई।
भारत के स्त्रीवादी पुरुष मित्रों को भी इस तरह के संगठनों की आवश्यकता महसूस हुई कि जिसमें, स्त्री आंदोलन का नेतृत्व स्त्रियाँ ही करें और हम उनकी मदद करें, उसमें सहभागी हों। 1985 में पुणे में मुकुंद किर्दंत की पहल पर ‘पुरुष उवाच’ नामक समूह गठित किया गया। इसी तरह मुंबई में हरीश सदानी और अन्य मित्रों ने 1993 में ‘मेन अगेंस्ट वॉयलेंस एण्ड एब्यूज़’ (MAVA) की स्थापना की। ये दोनों समूह लैंगिक संवेदनशीलता पर विश्वास करते हैं। अपने कार्यों के माध्यम से अपने इस विचार को समाज में फैलाने की वे कोशिश कर रहे हैं। ‘पुरुष उवाच’ अनेक अध्ययन मण्डल आयोजित करता है तथा प्रति वर्ष ‘पुरुष उवाच’ शीर्षक से एक पत्रिका का दीपावली विशेषांक प्रकाशित करता है, जिसमें पितृसत्ता, मर्दानगी, पुरुषत्व की अवधारणा को निरस्त कर, स्त्री-पुरुष समानता के विचार को मानने वाले पुरुषों की रचनाएँ सम्मिलित की जाती हैं। ‘मावा’ की ओर से ‘इंसानियत की राह पर पुरुषों का स्पंदन’ घोष-वाक्य लिखा हुआ ‘पुरुष-स्पंदन’ नामक दीपावली विशेषांक प्रकाशित किया जाता है।
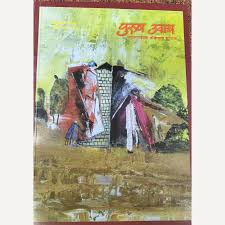
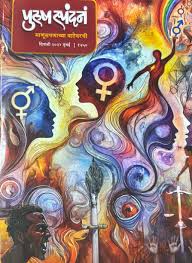
पितृसत्ता द्वारा प्रदान की गई स्त्री-पुरुषों की विभाजक भूमिकाओं के कारण एक इंसान की तरह विकसित होने में दोनों को बाधा और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। इन ढाँचों के कारण पुरुषों पर भी अनेक प्रकार के बंधन आते हैं। इनमें बदलाव लाने के लिए पुरुषों को पहल करनी पड़ेगी। ‘मावा’ महाविद्यालयीन युवकों के लिए कई कार्यक्रम निरंतर आयोजित करता है। ‘मावा’ के कार्यकर्ता, पुरुष द्वारा स्त्री को महज़ समर्थन प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं मानते, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि वे स्त्रियों के आंदोलन में बराबरी के साथ शामिल भी हों।
उपर्युक्त उल्लिखित सभी समूहों का विश्वास और अनुभव है कि पुरुष एक संवेदनशील मनुष्य है। परंपरा द्वारा लादी गई वर्चस्ववादी भूमिका का त्याग करने वाले पुरुषों में स्त्रियों के साथ होने वाली हिंसा को रोकने की क्षमता होती है। न केवल इस तरह के संगठनों से संबंधित पुरुष, बल्कि अपने आसपास के, नाते-रिश्ते के अनेक पुरुष ऐसे होते हैं, जो संवेदनशील और बदलने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे पुरुष माँ, बहन, सहेली, पत्नी, बेटी, कार्यस्थल की सहकर्मियों जैसी विविध संबंधों वाली स्त्रियों के जीवन में ख़ुशियाँ भरते हैं। वे उनकी मित्र होती हैं। पेर इस्डाल (Per Isdal) नामक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक का मत है कि “पुरुष को बदलना कठिन होने के बावजूद संभव है। हिंसा का विकल्प अहिंसक आचरण सीखते जाना ही है। अर्थात्, प्रतियोगिता की बजाय सहयोग, अनादर के स्थान पर आदर, तानाशाही की बजाय लोकतंत्र और समानता, चुप रहने या सिर्फ़ एक व्यक्ति के बोलते रहने की बजाय परस्पर संवाद, नियंत्रण के स्थान पर एकदूसरे को समझना, डर, नफ़रत, अपमान के स्थान पर प्रेम, सम्मान की ओर बढ़कर बदलाव लाया जा सकता है। साथ ही पुरुष को उसके द्वारा की जाने वाली हिंसा और तानाशाही को स्वीकार करने की ज़िम्मेदारी लेनी होगी।”
यह डर और हिंसा से मुक्ति की संयुक्त यात्रा है। स्त्रीवाद, स्त्री-मुक्ति पुरुष विरोधी नहीं है। स्त्री-पुरुष के बीच इंसानियत के रिश्ते की चेतना जागृत करने के लिए स्त्रीवाद का जन्म हुआ है। यह मानव-मुक्ति की यात्रा है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करने की बात जब समझ में आती है, तब यह यात्रा आसान हो जाती है, अपनी लगने लगती है।
हमारे देश में इस तरह के संवेदनशील और सहृदय पुरुषों की सुदीर्घ परंपरा और विरासत रही है। स्त्रियों को अध्यात्म का अधिकार प्रदान करने वाले वर्धमान महावीर, तथागत गौतम बुद्ध, भक्ति आंदोलन में संत मीराबाई की श्रेष्ठता को मान्यता देने वाली भक्ति-परंपरा, संत जनाबाई को सखा प्रतीत होने वाले संत ज्ञानदेव, नामदेव द्वारा निर्मित वारकरी परंपरा, अक्क महादेवी के वैराग्य और ज्ञान को समझकर क्रांतिकारी संत बसवेश्वर द्वारा स्थापित किया गया लिंगायत संप्रदाय जैसी सभी विद्रोही परंपराओं ने स्त्री-मुक्ति की राह तैयार करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचन्द विद्यासागर, महात्मा जोतिबा फुले, गोपाल गणेश आगरकर, महात्मा गांधी, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, इरोड वेंकट रामसामी पेरियार, महर्षि कर्वे जैसे पुरुष सुधारकों की दीर्घ परंपरा रही है। इन पुरुषों ने स्त्रियों की पीड़ा समझी, स्त्रियों के दुखों को सुना, उनके जवाब खोजे और उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश की। समाज में स्त्री-पुरुष समानता की चेतना जगाई। भारतीय पुरुषों को सामाजिक न्याय, सहिष्णुता और उदारता की इस विरासत को आगे बढ़ाना होगा।

पुरुषों में चेतना जागृत करने की ज़िम्मेदारी घर, स्कूल से लेकर शासन-संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं की भी है। घर का वातावरण, स्कूल का पाठ्यक्रम, राज्य-संस्थाओं की नीतियाँ सभी प्रकार की हिंसा और नफ़रत का विरोध करने वाली तथा लैंगिक समानता की पोषक होनी चाहिए, तभी पुलिस प्रशासन लड़कियों तथा स्त्रियों के साथ दहशतभरा व्यवहार नहीं करेगा। स्त्रियों की शिकायतें दर्ज की जाएंगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। माँट्रियल जैसा हत्याकांड कभी दोहराया नहीं जाएगा। लैंगिक समानता की ये यात्रा स्त्री-पुरुषों को मिलकर करनी होगी। इस तरह के प्रयत्न सामूहिक स्तर पर करने होंगे।
(यह लेख मुंबई से मराठी में प्रकाशित दैनिक ‘लोकसत्ता’ के 16 अगस्त 2025 के शनिवारीय परिशिष्ट ‘चतुरंग’ के पृष्ठ 03 पर प्रकाशित स्तंभ ‘स्त्री-आंदोलन के पचास साल’ के अन्तर्गत प्रकाशित है। ‘लोकसत्ता’ और मूल लेखक के प्रति आभार।)