(भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित कुछ ‘वाक्यांशों’ एवं ‘पदों’ पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। जैसे – “…समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सबमें व्यक्ति की गरिमा … सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए …” संकल्प लेने की बात कही गई है। संविधान लागू होने के 75 सालों बाद भी क्या इस संकल्प पर अधिकांश नागरिक अमल करते हैं? हमारी सामाजिक व्यवस्था में श्रेणीकरण और पदानुक्रम से उत्पन्न विषमता और वर्चस्ववाद सभी क्षेत्रों में झलकता है। कला के माध्यम भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। यहाँ फ़िल्मों में चित्रित ऐसे स्टीरियोटाइप्स की चर्चा की गई है, जो देश के आदिवासी समुदाय की संस्कृति को समझे बिना उसका मनमाना अक्स प्रस्तुत करते हैं। इनमें बहुत आसानी से कुछ समुदायों को ‘उन्नत’ और कुछ समुदायों को ‘पिछड़ा’ हुआ दिखाकर, उनकी ‘गरिमा’, ‘प्रतिष्ठा’ और ‘समानता’ के अधिकार को चोट पहुँचाई जाती है। संविधान लागू होने के 75 वर्षों बाद भी क्या हम ‘परस्पर सम्मान’ करने की भावना और विचार को आत्मसात नहीं कर पाए हैं? इस सवाल के इर्द-गिर्द विभिन्न समुदायों के सम्मान और बराबरी के अधिकार पर केंद्रित कुछ लेखकों के लेख और अनुवाद यहाँ साझा किए जा रहे हैं। इस कड़ी में पहला लेख है ‘भारतीय फ़िल्मों में आदिवासी छवि’।
फ़िल्मकार निरंजन कुमार कुजूर का यह लेख भारतीय फ़िल्मों में प्रस्तुत आदिवासी-चित्रण की इन्हीं विसंगतियों पर उँगली रखता है। निरंजन सत्यजीत रे फ़िल्म एण्ड टेलीविज़न इंस्टिट्यूट कोलकाता के स्नातक एवं बहुभाषी फ़िल्म निर्देशक हैं। आपने कुडुख़, संथाली, बांग्ला, हिन्दी तथा मेंडेरिन चाइनीज़ भाषा में फ़िल्में बनाई हैं। उनकी ‘एड़पा काना’ (Going Home), ‘पहाड़ा’, देबी दुर्गा, ‘तीरे बेंधो ना’, ‘खैका टुम्पा’ आदि फ़िल्में यूट्यूब पर देखी जा सकती हैं। उनके स्व-अनुभव में पगा यह लेख नए सिरे से विचार करने को बाध्य करता है। यह लेख लेखक की सहमति से ‘विश्वरंग’ (आदिवासी विशेषांक) के अप्रैल-जून, 2024 के अंक से साभार लिया गया है।)
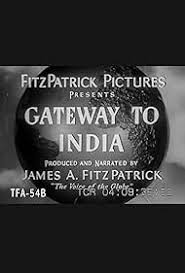
उन दिनों सत्यजीत रे फ़िल्म टीवी संस्थान में हमारी डाक्यूमेंट्री फ़िल्म की कार्यशाला चल रही थी। मुंबई से वरीय डाक्यूमेंट्री फ़िल्मकार, अविजित मुकुल किशोर जी इसके कर्णधार थे। वे हमें भिन्न-भिन्न प्रकार की डाक्यूमेंट्री फ़िल्मों और शैलियों से अवगत करा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले हमें 1930 में जेम्स ए फ़िट्ज़पैट्रिक द्वारा निर्मित एक ट्रैवलॉग फ़िल्म ‘द गेटवे टू इंडिया: बॉम्बे’ दिखाई। ज़ाहिर है, फ़िल्म भारतीयों के प्रति पश्चिम सभ्यता के नज़रिए को प्रस्तुत करती है। फ़िल्म के कुछ दृश्य और कमेंट्री ऐसी हैं कि एक भारतीय को कहीं ना कहीं अपमानजनक लग सकती हैं। जैसे शुरुआत में ही ताज होटल को देश की सबसे मिथ्याभिमानी बिल्डिंग कहा जाता है, वहीं एक दृश्य में शहर के बीचों-बीच भारतीयों को बैलगाड़ी दौड़ाते दिखाया जाता है और ठीक उसके बाद अंग्रेजों को मोटर कारें दौड़ाते दिखाया जाता है। इसी दौरान कमेंट्री में भारतीयों को पिछड़ा बताते हुए उन्हें 15वीं शताब्दी का और अंग्रेजों को 20वीं सदी का बताया जाता है। वहीं आगे चलकर फ़िल्म में भारतीय महिलाओं के पहनावे, साड़ी और माथे की बिंदी का वर्णन किया जाता है। पूरी फ़िल्म में फ़िल्मकार भारतीयों को ‘अन्य पुरुष’ के सर्वनाम से संबोधित करता है। मेरे सहपाठी इस बात की चर्चा करते रहे कि किस तरह उन दिनों भारतीयों को एक अजूबे की तरह ही देखा जाता था। परंतु उस वक़्त मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। मुझे आदिवासियों पर देश की मुख्यधारा के फ़िल्मकारों द्वारा निर्मित कुछ एंथ्रोपोलोजिकल फ़िल्में याद आ रही थी जिन्हें देखते हुए मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ‘ये लोग’, ‘इन लोगों को’, ‘इनका’ जैसे सर्वनाम यहाँ भी उपयोग में लाये जाते रहे हैं । यह ‘अन्य पुरुष’ का संबोधन है जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो बाहरी लोग एक ख़ास समुदाय के बारे में बातें कर रहे है। नरेशन का यह भाव आदिवासियों को अन्यीकरण की ओर ले जाता है।
नब्बे के दशक में जब भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर चल रहा था, तब उसका बहुत बड़ा बोझ आदिवासियों पर पड़ रहा था।औद्योगीकरण के लिये जबरन भूमि-अधिग्रहण, विस्थापन, पलायन के दंश से आदिवासी जूझ रहे थे। मैं डाक्यूमेंट्री फ़िल्मों की बहुत कद्र करता हूँ क्योंकि केवल वे ही आदिवासी मुद्दों को उस वक़्त उठाने का काम कर रही थीं, जब मीडिया इन मुद्दों को नहीं उठाती थी, अख़बारों में उन्हें जगह नहीं मिलती थी। डाक्यूमेंट्री फ़िल्मों ने तब अपने स्तर पर एक पैरेलल और वैकल्पिक मीडिया के रूप में काम किया और दुनिया के सामने विकास के नाम पर हो रहे विनाश के काले सच को सामने रखा। मीडिया जहाँ हम आदिवासियों को विकास-विरोधी या नक्सली करार दे रही थी, वहीं डाक्यूमेंट्री सिनेमा आदिवासियों की आवाज़ बन कर उभरा। मुझे इन फ़िल्मों से कोई शिकायत तो नहीं है, और शायद कभी हो भी नहीं सकती, लेकिन चूँकि बात आदिवासी-छवि के बारे में हो रही है इसीलिए इस पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। डाक्यूमेंट्री सिनेमा आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों की ओर सरकार और आम जनता का ध्यान खींचने में सफल रहा था। कई फ़िल्में पुरस्कृत भी हो रहीं थीं। लेकिन चूँकि आदिवासियों का ऑडियो-विज़ुअल मीडियम में इतने मुखर और वृहद् रूप से प्रतिनिधित्व पहले कभी नहीं हुआ था, तो आदिवासी लोगों के इस तरह बार-बार के चित्रण से उनकी एक आंदोलनकारी या बाग़ी क़िस्म की छवि बन गई। यह सब अनजाने में हुआ। इस प्रकार के मानसिक प्रभाव का अंदेशा किसी को नहीं था क्योंकि फ़िल्मकार पूरी शिद्दत से हमारे मुद्दों को उठाने में लगे थे।
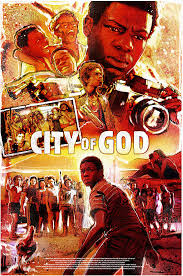
जब मैं फ़िल्म स्कूल गया तो सिर्फ़ मेरे आदिवासी होने की वजह से मेरे सहपाठी यह मान कर बैठे थे कि मैं डाक्यूमेंट्री फ़िल्मकार ही बनूँगा। वहीं मेरे एक प्रोफेसर ने मेरी पहली शॉर्ट फ़िक्शन फ़िल्म ‘पहाड़ा’ देख कर ये कहा कि “ये क्या बोरिंग ईरानी सिनेमा जैसी फ़िल्म बनाये हो? मुझे लगा तुम ‘सिटी ऑफ़ गॉड’ जैसा कुछ बनाओगे।” ‘सिटी ऑफ़ गॉड’ ब्राज़ील के सभ्य समाज से बहिष्कृत झुग्गियों में रहने वाले दो दोस्तों की कहानी है जिसमे से एक का सपना फोटोग्राफर बनने का है वहीं दूसरा बड़ा होकर ड्रग डीलर बन जाता है। तो समझ आता है की कहीं ना कहीं जागरूक प्रबुद्ध समाज भी आदिवासियों के प्रति किसी ना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। मुझे हमेशा इस बात का एहसास होता था कि कहीं ना कहीं सारी फ़साद की जड़ धारणाओं और भ्रांतियों का है, तभी लिखने, दिखाने में चूक हो रही है जो आदिवासियों का गरिमापूर्ण जीवन नज़र नहीं आ रहा हैं। आदिवासी एक सामुदायिक जीवन जीते हैं, जिनमें मानवीय संवेदनशील रिश्तों की अहम भूमिका होती है, फिर भी आदिवासियों का मानवीय रूप भारतीय फ़िल्मों में देखने को नहीं मिलती।
मैंने ऋत्विक घटक की ‘अजांत्रिक’ (1958) पहली बार 35 mm रील में हमारे फ़िल्म स्कूल के मेन थियेटर में देखी। तब मैं अपने कोर्स के फर्स्ट ईयर में ही था इसीलिए उनकी फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा अवगत भी नहीं था। मेरे बंगाली दोस्त उनको लेकर ख़ासे उत्साहित रहते थे। बहरहाल फ़िल्म शुरू हुई। कुछ समय बीतते ही अचानक दूर से कोरस में गीत के स्वर सुनायी देते हैं, जो जाने-पहचाने से लग रहे थे। फिर आगे चलकर गीत और प्रमुखता से आने लगते हैं। तब आपको समझ आता है कि ये तो कुँडुख भाषा के गीत हैं। फ़िल्म और आगे बढ़ती है और क्लाइमेक्स की ओर आते-आते उराँव ‘जतरा’ का दृश्य आता है। विधिवत पंक्तियों में नाचते – झंडा लिए परेड करते आदिवासी। हवा में लहराते आलीशान झंडे। पारंपरिक परिधान और वाद्य यंत्र, बड़े बड़े नगाड़े-माँदर, यह सब देख कर मन उत्साह और ख़ुशी से झूम रहा था। पारंपरिक परिधान हर आदिवासी समुदाय की अपनी पहचान से जुड़ा होता है और यह ध्यान देने वाली बात है कि ऋत्विक घटक ने उराँव आदिवासियों की अस्मिता से कोई समझौता नहीं किया। इसके अलावा आदिवासियों को ही आदिवासियों के भूमिका में कास्ट करना, उन्हें कुँडुख भाषा में संवाद देना, प्रेमी-प्रेमिकाओं के झगड़े, रोमांटिक छेड़खानियाँ वग़ैरह, इन सब में साफ़-सुथरी, गरिमामयी आदिवासी सिनेमा की संभावनाओं की एक झलक दिखती है।

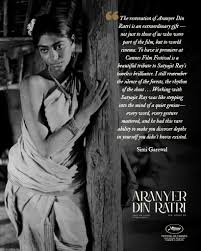
अब हम सत्यजीत रे द्वारा निर्मित फ़िल्म ‘अरण्येर दिन रात्रि’ (1970) पर आते हैं। इस फ़िल्म की कहानी में तीन जिगरी दोस्त छुट्टी मनाने पलामू के जंगलों में जाते हैं। फ़िल्म में एक आदिवासी किरदार है दुली, जिसे निभाया है सिमी ग्रेवाल ने। उनके गोरे चमड़े को मेकअप से काला बनाया गया ताकि वह आदिवासी दिख सके। फिर आप उनके चरित्र-परिचय वाले सीन में प्रथम इमेज के तौर पर उसे ठेके पर नशे की हालत में मद्यपान करते हुए और अनजान लोगों से ‘आधा पउआ’ शराब के लिए मिन्नतें करते हुए दिखाते हैं। दुली के संवाद टूटे-फूटे बांग्ला में हैं। हालाँकि रे ने यह फ़िल्म बंगाली भद्रलोक को आईना दिखाने के उद्देश्य से बनायी होगी, परंतु इस क्रम में आदिवासियों की छवि कहीं भी गरिमापूर्ण नहीं दिखती। फ़िल्म में आगे जब दुली अपने दो और साथियों के साथ उनके डाक-बंगले पर काम करने आती है, तब शेखर (रबी घोष) उनके सामने नंग-धडंग अवस्था में ही चले आते हैं। यही नहीं, जब दुली उनके कमरे की सफ़ाई कर रही होती है तब तीनों कमरे में ही होते हैं और उसे अश्लील नज़रों से ताड़ते हैं। बाद में वहाँ का केयर टेकर उन्हें “ये गंदी औरतें हैं साहब!” कह कर भगा देता है। इसके ठीक बाद ये कुएँ में नहा रहे होते हैं। उसी वक़्त शर्मिला टैगोर अपनी गाड़ी से वहाँ उनका खोया वॉलेट लौटाने आती हैं। अधनंगे देखे जाने के डर से ये हड़बड़ाते हुए गिरकर कुएँ की ओट में छिप जाते हैं। मुख्यधारा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सत्यजीत रे यहाँ बहुत ही अभूतपूर्व तरीक़े से बंगाली भद्रलोक को अधनंगा करके उनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाते हैं। यही इस सीक्वेंस की जीत है। पर वहीं अगर हम इसी सीक्वेंस को आदिवासी दृष्टिकोण से देखें तो यह इतना सुंदर नज़र नहीं आता है। सीक्वेंस आदिवासी महिलाओं के ऊपर ख़ुद को बेहतर समझने वाले समुदाय के मर्दों के कामुक दृष्टि को कहीं ना कहीं रेखांकित भी करता है। वहीं पूरी फ़िल्म में कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि आदिवासी मूल्य वास्तव में कैसे हैं। इस बात की कमी खलती है कि अप्रिय बनते चित्रण को बचाने हेतु रे आदिवासियों के लिए कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं करते। फ़िल्म जब अपने उत्कर्ष पर पहुँचती है तब, जतरा में हो रहे आदिवासी नाच-गान निरर्थक और अपूर्ण लगते हैं। तेज़ कट वाले इस सीक्वेंस में इनका इस्तेमाल केवल एक प्रकार का इफ़ेक्ट बनाने के लिए किया गया है ।
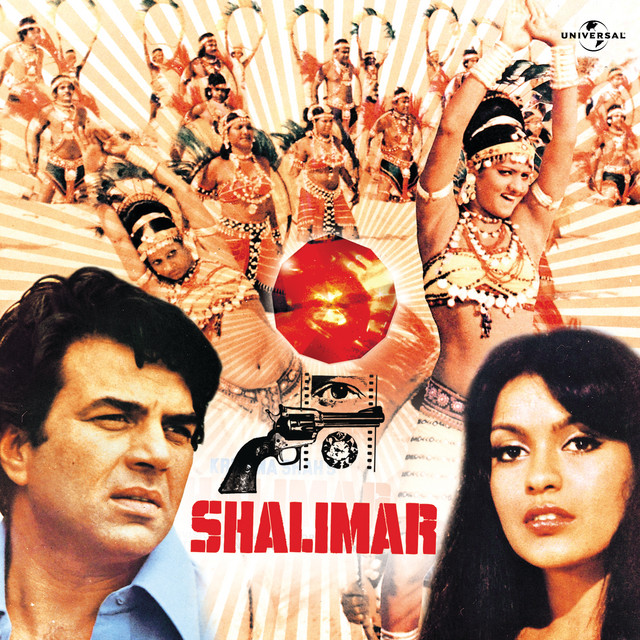
1978 में बनी ‘शालीमार’ तो सबको याद होगा। इस फ़िल्म में एक बहुचर्चित गाना था, जिसके बोल हैं – “हम बेवफ़ा हरगिज़ ना थे, पर हम वफ़ा कर ना सके”। इस गाने में बीच-बीच में आदिवासी “झींगा लाला हू, हुर्र हुर्र” करते हैं। इस फ़िल्म ने हमारी पीढ़ी के आदिवासियों को सीधी क्षति पहुँचाई है। स्कूल में आदिवासी बच्चों को ‘झींगा लाला हू’ कहकर सहपाठियों द्वारा चिढ़ाना, भाला लेकर नाचने वाला बताना, वग़ैरह। फ़िल्म में दुनिया के महानतम चोरों को एक द्वीप में प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस द्वीप का मालिक, जो कि मुख्य खलनायक भी है, वहाँ के आदिवासियों को अपने सैनिकों के रूप में रखा हुआ है। उनमें काले रंग के त्वचा वाले और उत्तर-पूर्वी नैन-नक़्श के अतिरिक्त कलाकार को मिलाकर इन्हें समरूप तरीक़े से पेश किया गया है। वहीं आदिवासियों का चित्रण अंधविश्वासी और ख़ूँख़ार लोगों के रूप में किया गया है। फ़िल्म के एक सीन में सर जॉन (रेक्स) कुमार (धर्मेंद्र) को ब्रांडी ऑफर करते हैं। धर्मेंद्र ब्रांडी का ग्लास लिए होते हैं और सर जॉन तीन आदिवासियों को सामने खड़ा कर उनपर राइफ़ल ताने उन पर गोली चला रहे होते हैं। सर जॉन उनसे बात करते हुए एक आदिवासी को गोली भी मार देते हैं और कुमार उनका बाथरूम इस्तेमाल करने की अनुमति लेकर निकल जाता है। पूरे सीन में उन आदिवासियों के बारे में कोई संवाद नहीं है, जिन पर सर जॉन शूटिंग का अभ्यास करते नज़र आते हैं। आदिवासी-जीवन के प्रति इतना मूल्यविहीन रवैया शायद ही कहीं देखने को मिले। इसके अलावा गीतों में आदिवासियों के डांस-स्टेप्स में उनसे उग्र मुद्राएँ करवायी जाती हैं, जबकि आदिवासी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गोलाकार चैन बनाते हुए नाचते हैं, जिसका मानसिक असर कुछ ऐसा होता है जिसमें पूरा समुदाय शांत और सुरक्षित महसूस करता है।
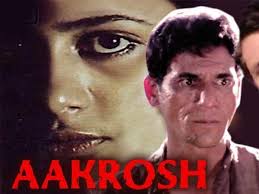
पैरेलल सिनेमा के विख्यात फ़िल्मकार गोविंद निहलानी जिन्होंने देश को ‘अर्धसत्य’ और ‘हज़ार चौरासी की माँ’ जैसी फ़िल्में दीं, उनकी बहुचर्चित फ़िल्म ‘आक्रोश’ (1980) की भी चर्चा हम कर लें। फ़िल्म में मुख्य किरदारों को निभाया है नसीरुद्दीन शाह, जो एक सरकारी वकील (भास्कर) बने हैं और ओम पुरी भिखु लहानिया की भूमिका में हैं जो एक आदिवासी है। भिखु अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ़्तार होकर पुलिस हिरासत में है, वहीं भास्कर उससे हमदर्दी रखता है; लेकिन उसके बिल्कुल जड़ हो जाने के कारण उसकी मदद कर पाने में ख़ुद को असमर्थ पाता है। फ़िल्म की कलात्मकता, सिनेमेटोग्राफ़ी बहुत प्रभावशाली हैं। फ़िल्म बड़ी ही संजीदगी से अपने समाज के विशेषाधिकार और क़ानून की व्यर्थता को दर्शाती है कि कैसे क़ानून कुछ शक्तिशाली लोगों की कठपुतली की तरह काम करता है, और इस पूरे तंत्र में एक आदिवासी अपने आपको कैसे अकेला पाता है। इस फ़िल्म में एक ख़ास सीन की मैं बात करना चाहता हूँ। रात का समय है, भिखु अकेला जेल में अँगड़ाइयाँ लेते हुए कराह रहा है। फ़िल्म वहीं से फ़्लैशबैक में जाती है और हम भिखु को पत्ते के दोने में मद्यपान करते देखते हैं। भिखु की पत्नी (स्मिता पाटिल) शाम को देर से घर लौटती है। इस पर भिखु ग़ुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाता है। हालाँकि भिखु का ग़ुस्सा इसलिए नहीं था कि उसकी पत्नी देर से लौटी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसको इस बात का एहसास था कि उसके मालिक की उसकी पत्नी पर गंदी नज़र है। अमूमन फिक्शन फ़िल्मों में हम जानते हैं कि उसमें दिखाए गए एक-एक दृश्य, एक-एक ध्वनि चुनी हुई होती है। फ़िल्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको फ़िल्मकार बिना सोचे-समझे शामिल करते हैं। हम देख सकते हैं कि जब आदिवासियों के चरित्र-चित्रण की बात आती है तब अनायास ही नकारात्मक छवियाँ फ़िल्मकारों के ज़हन में उभर आती हैं। भिखु एक ऐसा पति भी हो सकता था जो शराब नहीं पीता था और जो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम से पेश आता था। ग़ौरतलब है कि बार बार आदिवासियों के प्रति जो सामाजिक रूढ़िबद्ध धारणाएँ हैं, भारतीय सिनेमा उसी को बार-बार अपने दर्शकों के बीच परोस रहा है। नतीजतन ये नकारात्मक धारणाएँ टूटने के बजाए और मज़बूत हो जाती हैं।

बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपयों का व्यापार करने वाली एस. राजमौली की फ़िल्म ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ में कलाकेया नाम की एक काल्पनिक जनजाति की रचना की गई। इस पर बहस की जा सकती है कि वो आदिवासी हैं या नहीं लेकिन कुछ ख़ास बिंदुओं पर नज़र डालें तो इनके आदिवासी होने की पुष्टि की जा सकती है। सबसे पहले तो इन्होंने एक पूरी भाषा ही बना डाली, जिसका नाम किलिकी या किलकिली रखा गया। भाषा के रचनाकार मदन कार्की बताते हैं कि उन्होंने इस भाषा की शुरुआत माउस के क्लिक की आवाज़ से की। जबकि यह सर्वविदित हैं कि अफ़्रीका महादेश में नामीबिया, बोत्स्वाना, दक्षिणी अफ़्रीका जैसे देशों में अनेक आदिवासी भाषाएँ हैं जिनमें क्लिक व्यंजन समाहित हैं। इस भाषा-परिवार को खोइसान कहा जाता है। खोइसान के अलावा कई बंटू भाषाएँ (जैसे ज़ुलू ) भी क्लिक व्यंजन का इस्तेमाल करती हैं। फ़िल्म में इनकी रूप-सज्जा को देखें तो आपको वही राक्षसी चित्रण नज़र आएगा, जो महाकाव्यों, धार्मिक सीरियल वग़ैरह में कई अरसों से आदिवासियों का होता आ रहा है। काला रंग, मैले-कुचैले बाल और शरीर, दानवी हुलिया, वग़ैरह। उनके हथियार, जैसे कि दानवी तलवार, कुल्हाड़ी, भाला आदि भी बुनियादी नज़र आते हैं। बुनियादी हथियार बनाम अत्याधुनिक हथियार वाले युद्ध आदिवासी क्षेत्रों में आम तौर पर देखे जाते रहे हैं। पुलिस की गोलियाँ बनाम तीर-धनुष, कुल्हाड़ियाँ या पत्थर। बाहुबली और भल्लाल देव की सेना जब कलाकेयाओं से लड़ते हुए जब अपने अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करते हुए उन्हें गाजर-मूली की तरह काट रही होती है, तब सिनेमा-हॉल में दर्शक तालियाँ और सीटियाँ बजा रहे होते हैं, और इस प्रकार आदिवासियों के जनसंहार का दर्शकों के अचेत मन में सामान्यीकरण कर दिया जाता है।

देबाशीष माखीजा की फ़िल्म ‘जोरम’ के मुख्य भूमिका में मनोज वाजपेयी हैं और वह ‘दसरू केरकेट्टा’ का किरदार निभा रहे हैं। ‘केरकेट्टा’ गौरैया चिड़िया की प्रजाति है और इस टोटम के लोग झारखण्ड के उराँव, मुण्डा और खड़िया समुदाय से आते हैं। जैसा कि हमने ‘अजांत्रिक’ में जाना कि किस प्रकार ऋत्विक घटक ने उराँव आदिवासियों की रूप-सज्जा और पारंपरिक परिधान के प्रति ख़ास ध्यान रखा, माखीजा की ‘जोरम’ में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। उल्टे नियमगिरी (ओड़िशा) के डोंगरिया कोंध के परिधान और रूप-सज्जा को इन पर चिपका दिया गया है। यह ठीक वैसा है जैसे मानो किसी तमिल किरदार को पंजाबी परिधान दे दिये हों। चूँकि डोंगरिया कोंध भारत का एक मात्र ऐसा आदिवासी समुदाय है, जो गत वर्षों वेदान्त के ख़िलाफ़ अपने नियमगिरी देवता को बचाने की लड़ाई के कारण दुनिया भर में सुर्ख़ियों में रहा। ऐसा लगता है फ़िल्मकार ने उसी अंतरराष्ट्रीय तस्वीर को भुनाने की कोशिश की। फ़िल्म शोध के मामले में बेहद कमज़ोर नज़र आती है। ऐसा लगता है कि फ़िल्मकार ने झारखंड-भ्रमण किये बग़ैर केवल गूगल के माध्यम से जो तस्वीरें निकल पायीं, उसी को आधार बनाकर ये फ़िल्म बना डाली। एक दृश्य में मनोज वाजपेयी मुंबई से भाग कर अपने गाँव के पास के इलाक़े में पहुँचते हैं। वहाँ वह पथलगढ़ी आंदोलन के प्रतीक, ग्राम सभा की शक्तियों का उल्लेख करती मेगालिथ, के नीचे अपने नवजात शिशु को गोद में लिये बैठे नज़र आते हैं। पथलगढ़ी आंदोलन मुण्डा आदिवासियों का है, और इस प्रकार के पथलगढ़ी केवल मुंडा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ फिर एक बार झारखंडी गूगल तस्वीर को भुनाया गया है।

फ़िल्म में आगे एक आदिवासी को आप ‘लौंडा नाच’ करते भी देखते हैं। आपको बता दूँ ‘लौंडा नाच’ बिहार की संस्कृति का हिस्सा है, और इसका झारखंड से कोई सरोकार नहीं है। अगर झारखंड में छिटपुट कभी रिपोर्ट भी हो जाये तो वह आदिवासी समुदाय के बीच का नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसको फ़िल्म में आइटम नंबर के हिसाब से डाला गया है। ‘इंडी (स्वतंत्र) फ़िल्में’ आम तौर पर शोध की पक्की होती हैं और इस प्रकार के बाज़ारी दबाव में नहीं आतीं, ‘जोरम’ इस मामले में अपवाद है। फ़िल्म रोटरडैम और बुसान जैसे फ़िल्म महोत्सव में चयनित हो चुकी है और इसे वर्ष 2024 का फ़िल्म फेयर बेस्ट फ़िल्म (क्रिटिक्स) के साथ-साथ बेस्ट स्टोरी का फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है।
आदिवासी-चित्रण में त्रुटियाँ ज़्यादातर पूर्वाग्रह, स्वयं का श्रेष्ठता-बोध और अपरिपूर्ण शोध की वजह से आ रहीं हैं। फ़िल्मकार अगर ग़ैर आदिवासी है तो इन सब बाधाओं को पार पाने का अतिरिक्त प्रयास नहीं करता। आदिवासियों को पिछड़ा समझने के स्थान पर उन्हें एक समानांतर सभ्यता के तौर पर समझने की आवश्यकता है। एक सभ्यता, जिसका दर्शन, अर्थशास्त्र, अध्यात्म, पर्व-त्योहार, प्रशासनिक व्यवस्था, पारंपरिक परिधान, ख़ान-पान मुख्यधारा की सभ्यता से भिन्न है। जैसे, आज की मुख्यधारा नक़द पूँजी पर केंद्रित है जबकि आदिवासी समाज भूमि को असल पूँजी समझता है। कल अगर बैंकिंग तंत्र का पतन होता है तो पूरी मुख्यधारा धरातल पर आ जाएगी, चारों तरफ़ लूट-हत्या का माहौल रहेगा, लेकिन ज़मीन आदिवासियों की जाँची-परखी हुई पूँजी है, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पाल-पोस रही है। उसी प्रकार देखें तो आदिवासी, जो कि हज़ारों वर्षों से नकद-विहीन अर्थव्यवस्था के साथ जीवित रहा है; ज़ाहिर है हमारा विवेक और जीवन-शैली वैकल्पिक साधनों का बेहतर उपयोग करना जानता है। जैसे हमारी व्यवस्था में लोग एक दूसरे की मदद करते हुए चलते हैं। मैं आपकी फसल काटने में मदद करूँ, आप मेरी करेंगे; मैं आपका घर बनाने में मेहनत करूँ, आप मेरे घर को बनाने में मदद करेंगे। कई अवसरों पर हम एक साथ मछली पकड़ने जाते हैं, जब मछली पकड़ना हो जाता है तो वह पूरे गाँव में बराबर बाँटी जाती है। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, संसाधनों में हिस्सेदारी को तरजीह दी जाती है। ज़ाहिर है इससे मानवीय सम्बन्ध मज़बूत होते हैं, और एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव बना रहता है। लेकिन सिनेमा में आदिवासियों की मानवीयता को जगह नहीं दी जाती। अगर इन आदिवासी-मूल्यों पर आपका ध्यान नहीं जाता तो आप आदिवासियों के विरुद्ध पक्षपाती विचारों से ग्रसित हैं। आदिवासियों का चित्रण वैसा ही करें जैसा कि आप ख़ुद चित्रित होना चाहते हों क्योंकि आदिवासियों पर सिनेमा रोज़-रोज़ नहीं बनता।





निरंजन भाई को इस बेहतरीन आलेख के लिए दिल से शुक्रिया। आलेख न सिर्फ तथ्यपरक है अपितु सामयिक भी है।