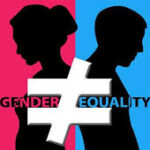मूल मराठी लेखिका : मंगला सामंत
(मणिपुर में दो महिलाओं के साथ पुरुषों की भीड़ द्वारा जो क्रूर आचरण किया गया, उसका अभी-अभी वीडियो वायरल होने के कारण समूचे संवेदनशील लोगों में तीखे क्षोभ और आक्रोश की लहर उठी है। महिलाओं के साथ इस तरह की अमानवीय हिंसक घटनाएँ जब भी घटती हैं, हम सब बहुत आहत, व्यथित और चिंतित हो जाते हैं। इस तरह का अमानवीय व्यवहार सभ्यता के इस चरण पर पहुँचने के बाद भी आखिर क्यों होता है, इसका सामाजिक मनोविज्ञान तलाशने की कोशिश करती रही हूँ। इस लेख में इसी विचार पर कुछ तथ्य और सन्दर्भ प्रस्तुत किये गए हैं। हालाँकि इस लेख में सिर्फ स्त्री-पुरुष इन दो लिंगों पर ही विचार किया गया है, परन्तु भिन्न लिंगीय व्यक्तियों के साथ होने वाली हिंसा और असमानता के मूल में भी यही विश्लेषण लागू हो सकता है। मूल मराठी लेखिका मंगला सामंत और ‘मिळून साऱ्याजणी’ मासिक पत्रिका की संपादक गीताली के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। लेख कुछ बड़ा होने के कारण दो कड़ियों में साझा कर रही हूँ। – उषा वैरागकर आठले)
पिता के निर्धारण के लिए स्थापित की गयी विवाह-संस्था ने पुरुष को असीमित सत्ता प्रदान की। इसके कारण महिलाओं और बच्चों को पुरुष की तानाशाही और हिंसा का सामना करना पड़ा। महिलाओं पर होने वाली हिंसा के जटिल सवाल को सुलझाने के लिए ‘जैसे को तैसा’ न्याय के अंतर्गत पुरुष के प्रति आक्रामक रुख़ अपनाकर महिला का हिंसक होना कोई उपाय नहीं है। बल्कि इससे पूरे परिवार के तहसनहस होने का खतरा है। शारीरिक बल के आधार पर किसी समस्या का समाधान करने की पहल से किसी का भला नहीं होगा। परिवार को जीवन-संघर्ष में टिकाये रखने के लिए ममता, प्रेम, विश्वास, परस्पर समझदारी और संवेदनशीलता जैसे पारिवारिक मूल्यों की ज़रुरत है। महिलाओं को समता, स्वतंत्रता और स्व-रक्षा के लिए आक्रामक और हिंसक होने की बजाय, पुरुषों द्वारा अपना अहंकार और आक्रामक वृत्ति छोड़कर परिवार के नाते-रिश्ते सहेजने के लिए अपने भीतर पारिवारिक मूल्यों को विकसित करने की ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। एक बेहतर प्यारा परिवार-केंद्रित पिता होने के लिए यह बदलाव बहुत ज़रूरी है। इसी कोशिश के एक हिस्से के लिए ‘साऱ्याजणी’ पत्रिका की विदुषी साथी का यह लेख पितृ-दिन के अवसर पर प्रस्तुत है।

‘सशक्तीकरण’ शब्द के साथ तुरंत जुड़ने वाला शब्द ‘महिला’ है। हम सब इससे वाक़िफ़ हैं क्योंकि हमारे मन में पीढ़ी-दर-पीढ़ी से यह बात गहराई तक पैठी हुई है कि, ‘पुरुष बलशाली होते हैं और महिलाएँ अबला होती हैं।’ सशक्तीकरण की व्याख्या ही पुरुष वर्ग के पैमाने पर की गई है। 8 मार्च को महिला दिन के अवसर पर तो महिला सशक्तीकरण के उपायों पर चर्चा की, महिलाओं को सम्मानित करने की, उन्हें पुरस्कार या छूट प्रदान की समूची मर्दानी दुनिया में ऐसी होड़ लगी रहती है कि दिल बाग़-बाग़ हो जाता है। इसलिए पुरुष को भी सशक्त करने की ज़रूरत है, यह विचार किसी के भी दिल-दिमाग़ को कैसे छू सकता है! हालाँकि महिला दिन के अगले दिन से ही फिर एक बार महिलाओं को कमतर मानने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो जाता है।
पिछले हज़ारों सालों से अनेक प्रकार के उपाय, कपट व षड्यंत्र रचकर, बेवकूफ़ बनाते हुए बहुत चालाकी के साथ महिलाओं को पुरुषों से पीछे रखा गया है। महिला दिन के वार्षिक आयोजन मात्र से वे सशक्त हो जाएँगी, इसका भुलावा देना इस सदी में महिलाओं के साथ दूसरा सबसे बड़ा धोखा है। आज तक पूजा-पाठ, धर्म-कर्म-उपासना की राह पर, अमुक उपवास से बच्चा होगा, तमुक व्रत से लड़का होगा, बरगद के फेरे लगाने पर यही पति अगले जनम में मिलेगा जैसे ढकोसलों से महिला समाज को धर्मबद्ध और मूर्ख बनाया जाता रहा है। उच्च शिक्षित महिलाएँ भी इस अंधश्रद्धा की चंगुल से नहीं बच पाई हैं। तो फिर किसी त्यौहार की तरह साल में एक बार मनाए जाने वाले महिला दिवस पर उनके जीवन का समग्र विचार और बीते साल की उनकी परिस्थितियों का कठोर परीक्षण करने की बजाय नई साड़ी या आधुनिक कपड़े पहनकर, एकदूसरे को ‘हैप्पी दशहरा’ कहने की तरह सहजता के साथ शुभकामनाएँ देना क्या कहला सकता है? क्या वह ‘सावन महीने का कोई एक त्यौहार’ मात्र बनकर नहीं रह जाता है?
पिछले तीन हज़ार वर्षों से पारिवारिक, सामाजिक तक़लीफ़देह स्थितियों व संस्कारों के कारण जो वैचारिक और बौद्धिक जड़ता महिलाओं के मस्तिष्क पर छा गई है, उसके परिणाम अभी भी नियंत्रण में नहीं आ पाए हैं। पहले से ही बहुसंख्य महिलाओं के पास अपने हाथ-खर्च के लिए भी पैसे न होने के कारण, त्यौहार के अवसर पर कुछ चीज़ें हासिल कर लेने की पारम्परिक आदत के कारण, साथ ही किसी ख़ास दिन महिलाओं को कुछ देने का दिखावा कर, साल भर की गई उनकी बेइज़्ज़ती को भुला देने का भ्रम पैदा करने की पुरुष की चालबाज़ी के कारण महिलाओं के सार्वभौमिक न्याय का संघर्ष ज़ोर नहीं पकड़ पाता। इसीलिए सालों-साल कितने भी महिला दिन क्यों न मना लिये जाएँ, महिलाओं के सवाल, उनके साथ होने वाले अन्याय-अत्याचार व अपमान को कम नहीं किया जा सका है।
इसके लिए बतौर एक उपाय, महिलाओं के स्थान पर पुरुष के ‘सशक्तीकरण’ पर विचार करने से क्या परिस्थितियों में कोई फ़र्क़ आने की संभावना पैदा हो सकती है, यहाँ यही देखने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सबसे पहले सशक्तीकरण का आशय समझना होगा। किसी भी प्राणी के जीवन-संघर्ष में, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसे जो दाँवपेंच, प्रयास करने पड़ते हैं या जिन गुणधर्मों को उसे अपनाना पड़ता है, उसी ‘आत्मसातीकरण’ को सबलीकरण कहा जा सकता है। ज़िंदा रहने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास करना हरेक प्राणी-मात्र की विशेषता होती है। यह नैसर्गिक देन होती है। इसके कारण ही प्राणी-जगत जीवित रहता है। प्राणी-मात्र में, उसके विकास-क्रम के विभिन्न चरणों में, उसमें होने वाले मस्तिष्क के क्रमिक विकास में, उसके आसपास की जीवन-स्थितियों में, उसमें होने वाले बदलावों में; इसी तरह अगर वे जलचर हैं, थलचर हैं या वायुचर हैं, उसके अनुसार उनके ‘टिके रहने’ की क्षमता और कुशलता पृथक-पृथक होती है, परंतु सिद्धांत एक ही होता है – ‘किसी भी तरह जीवन-संघर्ष में ज़िंदा रहें’। अब इस सिद्धांत के अनुसार महिलाओं को शक्तिशाली बनाने की कोशिशें आखिर किसके साथ मुकाबला करने के लिए हो रही हैं? प्रकृति द्वारा ‘ताक़त के साथ जीने के लिए’ मनुष्यमात्र को ही, अर्थात पुरुष की तरह महिलाओं को भी सभी प्रकार की क्षमताएँ प्रदान की गयी हैं। इसके बावजूद आज महिला को ‘टिके रहने के लिए’ सबसे महत्वपूर्ण संकटग्रस्त सवालों से क्यों जूझना पड़ता है?
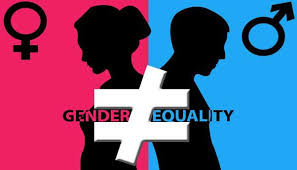
कुल मिलाकर जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और फिर परिवार की अवस्था में विकसित होने तक, मनुष्य के ‘टिके रहने की’ संकल्पना और प्रयासों में बदलाव आते चले गए। वह अन्य प्राणियों की तरह महज़ प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीने की बजाय बुद्धि-प्रामाण्यवादी प्रयत्नों से विकसित होता चला गया। स्त्री को अपनी प्रसूति के लिए और बच्चों के पालन-पोषण के लिए सबसे पहले स्थिरता की आवश्यकता महसूस हुई और वह आग की खोज के बाद गुफा में बस गई। इस मामले में स्त्री ने अपनी बुद्धि का उपयोग, अपनी संतान के साथ परिवार को ‘टिकाए रखने के लिए’ किया, यह कहा जा सकता है। यहाँ से जंगली युग का अस्त होकर बर्बर युग की शुरुआत होती है। साथ ही मातृप्रमुख टोली-व्यवस्था के काल का आरम्भ भी माना जाता है। बर्बर युग में आग के कारण आई स्थिरता के कारण स्त्री को अपनी संतान का सान्निध्य प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप स्त्री में परिवार के प्रति वात्सल्य का भाव उदित हुआ और वह मातृ-टोली परिवार बनाने की ओर अग्रसर हुई। अगली अनेक सदियों में अपनी संतान के सान्निध्य के कारण स्त्री का जंगली हिंस्र रूप घटता चला गया और उसमें ममता, प्रेम, वात्सल्य, संवेदना, भद्रता के गुणों का पोषण होता चला गया, जो विकसित होने वाले तत्कालीन नए परिवार को टिकाये रखने के लिए उपयुक्त था। इस तरह बदलती परिस्थितियों के कारण स्त्री-जाति का नए सिरे से प्राकृतिक सशक्तीकरण होता चला गया। मगर दूसरी ओर, पुरुष उसी तरह जंगली घुमंतू अवस्था में ही रह गया। संतान होने में अपने योगदान के बारे में उसे कोई ज्ञान न होने के कारण बाल-बच्चों के साथ रहने वाली मानसिकता उसमें विकसित नहीं हो पाई। यह बात जंगली युग, बर्बर युग से लेकर संस्कृति युग के उदय की अनेक सदियों तक पुरुष नहीं जानता था। स्तनधारी नर-पशु की तरह ही पुरुष की अपने परिवार और संतान से कोई प्रतिबद्धता नहीं थी।
सुप्रसिद्ध सेक्स थेरेपिस्ट थेरेसा क्रेन्शाव अपनी किताब The Alchemy of Love and Lust में लिखती हैं, ‘जो हार्मोन स्त्री के गर्भाशय में पुरुष को गढ़ने का काम करता है, उस ‘टेस्टॉस्टेरॉन’ हार्मोन के परस्पर प्रतियोगिता, ईर्ष्या, बदला लेने की प्रवृत्ति, साहस, आक्रामकता जैसे परिणाम अन्य स्तनधारी प्राणियों की तरह पुरुष में भी दिखाई देते हैं।’ जंगली युग में घुमन्तू अवस्था में भटकते हुए, इस प्राकृतिक आक्रामक प्रवृत्ति का उपयोग संघर्ष में खुद की रक्षा करने, खुद को ज़िंदा बचाए रखने के लिए आवश्यक था। आक्रमणकारियों का सामना कर उन्हें खदेड़ने के लिए अनेक दाँव-पेंच अपनाने पड़ते थे। जंगल का शासन प्रतियोगिता पर ही टिका रहता था। इसके लिए उसे अन्य जंगली पुरुषों या टोलियों के सामने ‘टिके’ रहकर जीवित रहना महत्वपूर्ण था। इसीलिए पुरुष की आक्रामकता, हिंसकता जैसी विशिष्ट प्रवृत्तियों को उसकी जंगली स्थिति के लिए स्वाभाविक ‘प्राकृतिक सशक्तीकरण’ कहा जा सकता है। सारांश यह कि, पुरुष और स्त्री, बर्बर युग से संस्कृति युग तक की कुछ सदियों में, क्रमशः बर्बर जीवन और पारिवारिक जीवन जैसी दो भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का सामूहिक जीवन जी रहे थे। यह वास्तविक स्थिति है।
आगे चलकर संस्कृति युग में विवाह-संस्था की शुरुआत होने से पुरुष का बर्बर जीवन समाप्त हुआ। तब उसमें विद्यमान हिंस्र-रूप का उपयोग धीरे-धीरे कम होते जाने के कारण ‘बर्बर सशक्तीकरण’ की प्रवृत्ति भी कमज़ोर पड़ने लगी। जिस समय पारिवारिक सहजीवन में परिवार के प्रमुख को समूचे पारिवारिक समुदाय की ज़िम्मेदारियों को समझदारी के साथ निभाना होता है, उस समय बदले की भावना, आक्रामकता, दुस्साहस जैसे बर्बर शक्ति के पैमाने, परिवार के स्थापित होने की दृष्टि से अनुपयोगी, बल्कि नुक़सानदेह ही साबित होते हैं। अर्थात, पारिवारिक जीवन को सुरक्षित रखने वाले और संघर्ष में टिकाये रखने वाले ममता, संयम, संवेदना, अच्छे-बुरे की पहचान का विचार, सहकार्य, त्याग आदि गुण पुरुष में उनकी साहसी प्रवृत्ति तथा विशेषताओं के साथ अंकुरित करने और पुष्पित-पल्लवित करने को ही पुरुषों का अपेक्षित सशक्तीकरण कहा जाना चाहिए था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि, पुरुष को उसके मूल आक्रामक गुणधर्मों से परावर्तित करने का प्रयत्न, मात्र कुछ आदिम जनजातियों में किया गया। माली नोवास्की ने अपनी किताब The Sexual Life of Savages में एक जनजाति के बारे में अपने शोध-परिणामों की चर्चा की है। आदिम अवस्था में रहने वाले टोब्राइंड नामक अफ्रीकन जनजाति में निष्ठा के साथ लम्बी अवधि तक एक साथ रहने वाले स्त्री-पुरुष में, जब स्त्री गर्भवती हो जाती थी और दोनों की इच्छा और सहमति होती थी, तो पुरुष को उस होने वाले बच्चे का अभिभावकत्व कुछ शर्ते पूरी करने पर ही प्रदान किया जाता था। मुख्य शर्त थी कि, उस पुरुष को अगले छै महीने हर प्रकार की हिंसा से परे रहकर दिखाना होगा। वह घर से बाहर नहीं जाएगा, शिकार नहीं करेगा, लकड़ी या पेड़ या घास नहीं काटेगा। अपनी स्त्री की प्रसूति सम्पन्न होने तक उसे लेटे रहना पड़ेगा। उसके बाद ही खुद पर इतना नियंत्रण रख सकने वाला पुरुष ‘पिता’ के पद के लिए पात्र माना जाता था। इस पद्धति से उस समय के हिंसक पुरुष को शांत बनाने वाला जनजाति का प्रामाणिक प्रयास इसमें देखा जा सकता है। उस जनजाति द्वारा पुरुष के साथ किया जाने वाला यह प्रयत्न ‘विवाह प्रथा’ के रूढ़ होने के पहले का है। इस उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि, परिवार की एक इकाई के रूप में पुरुष को समाविष्ट करने से पहले वह नर-स्वभाव के अनुसार मूलतः हिसा की ओर प्रवृत्त होने के कारण, उसे ‘माँ-बच्चे’ के परिवार में सीधे प्रवेश देना ख़तरनाक़ साबित हो सकता है, यह वास्तविकता बाद में विवाह-प्रथा के आगमन-काल में बुद्धि-विकास के संस्कृति-काल के दौरान समूचे मानव-जाति को समझ में आनी चाहिए थी। परंतु इसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की।
अन्वेषकों का कहना है कि, विवाह-प्रथा के शुरु होने से पहले, आदिम अवस्था से बर्बर अवस्था के बीच दो युगों का काल-खंड लगभग एक लाख साल का था। उस काल में सदियों तक जंगली अवस्था में ‘टिके’ (सर्वाइव) रहने के लिए पुरुष द्वारा आक्रामक शैली के बर्ताव का सहारा लिया गया, जो उनके कठिन और असुरक्षित जीवन के परिप्रेक्ष्य में सही कहा जा सकता है। परंतु बाहरी दुनिया में, आज़ाद घूमते हुए आक्रामकता का, सत्ता का, अहंकार शांत करने का जो स्वच्छंद अवसर पुरुष को उस काल में मिलता था, उस स्वच्छंदता पर विवाह-संस्था का स्वीकार करने के बाद के काल-खंड में पुरुष पर अचानक बंधन आ गए। बंधन या स्वतंत्रता को मनुष्य तुरत-फुरत स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए समाज में विवाह-बंधन समग्रता के साथ सभी जगहों पर स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बावजूद, संस्कृति युग में, जिन-जिन समुदायों द्वारा उसे क्रमशः स्वीकार किया गया, उनमें मृदु व्यवहार की कोई भी शिक्षा (उपर्युक्त वर्णित टाब्राइंड जनजाति की तरह) अगर पुरुष को नहीं दी गई होगी, तो पुरुष में पीढ़ी-दर-पीढ़ी से रची-बसी आक्रामक जीवन-शैली में, बिना किसी शिक्षा-संस्कार के, जल्दी बदलाव होना असंभव था। और फिर, टोली मतलब पुरुषों का एक समूह, जिसमें बाहर से भागाकर लाई गई स्त्रियों का समावेश होता था। टोली-जीवन में एक प्रमुख पुरुष और शेष सभी स्त्री-पुरुषों की दोयम सदस्यता जैसी व्यवस्था होती थी। इसके बारे में फ्रेडरिक एंगेल्स अपनी किताब Origin of Family and Private Property में लिखते हैं, ‘फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति पुराने रोमन शब्द ‘फैमिलिया’ से हुई है और उसका अर्थ है, the number of slaves belonging to one man. प्रतीत होता है कि, टोली-अवस्था के पुरुष की कल्पना से उपजी ‘परिवार की कल्पना’ (Family Concept) पुरुष को सबसे पहले ‘मालिक’ मानकर ही कल्पित की गई। स्वाभाविक रूप में परिवार विषयक पुरुष की मूल मानसिकता स्वयंकेन्द्रित और टोली से उपजी हुई है। यह बात एंगेल्स के वक्तव्य से ज़्यादा स्पष्ट होती है। इसके विपरीत, जन्मदात्री स्त्री की परिवार संबंधी कल्पना ‘संतानकेन्द्रित’ होती है। स्त्री-पुरुष की मानसिक संरचना के इस बहुत बड़े अंतर का हमें ध्यान रखना होगा।

टोली कभी भी जन्माधारित व्यवस्था पर नहीं चलती थी, बल्कि किसी ताक़तवर, क्रूर पुरुष के वर्चस्व तले रहती थी। या फिर, किसी पुरुष के विद्रोह के कारण दोफाड़ होकर एक से दो टोलियों में बँट जाती थी। एक परिवार की तरह पिता, बेटे, पोते जैसी जन्म आधारित श्रृंखला का उसमें अभाव होता था। परिवार नाते-रिश्ते पर आधारित होता है और ‘टोली’ सिर्फ अपने बचाव और सत्ता की भावना से प्रेरित होती है। इसके कारण ही, परिवार को जीवन-संघर्ष में टिकाए रखने के लिए ममता, प्रेम, विश्वास, संवेदना जैसे मूल्यों की परम्परा टोली में विकसित नहीं हो सकती। टोली इन मूल्यों पर ‘टिकी’ नहीं रह सकती। परंतु, मातृ-परम्परा पर आधारित टोली के अनुसार जीने वाली समकालीन स्त्री, उसकी बच्चे को जन्म देने की क्षमता ही उसे उस परिवार की कल्पना से तत्काल जोड़ती है। जहाँ बच्चे का जन्म है, वहाँ स्त्री है ही। इसीलिए वहाँ परिवार भी है। अल्पावधि के लिए ही क्यों न हो, अन्य प्राणियों की माताओं में भी परिवार दिखाई देता है। इनमें पिल्लों के लिए ख़तरा बनने वाले नर को, वह प्रवेश भी नहीं करने देती। परिवार की धारणा बाबत स्त्री की शारीरिक, मानसिक, भावनिक संरचना पुरुष की तुलना में काफी पुरानी है, यह बात उपर्युक्त विवेचन से समझी जा सकती है। पुरुष का पितृत्व प्राकृतिक रूप से अज्ञात होने के कारण उसमें इस पारिवारिक भावना का नैसर्गिक अभाव होता है। इसीलिए, बाद में परिवार के लिए पोषक गुण आत्मसात करने में भी स्त्री की तुलना में पुरुष पिछड़ा रहता है। शायद इस बात को मानकर ही हमने इस बात की अब तक कोशिश नहीं की कि, पुरुष में इस तरह के सशक्तीकरण संबंधी मूल्यों का संस्कार करने पर विचार करना होगा। इसी तरह, पिछली अनेक सदियों से, बच्चे का पितृत्व अज्ञात होने के बावजूद, जिस स्त्री के कारण परिवार-व्यवस्था प्राचीन काल से टिकी रही, उसी स्त्री के साथ हिंसा, बलात्कार किया जाना, उसे घर-परिवार छोड़ने के लिए बाध्य करने जैसी घटनाएँ आज भी घट रही हैं। ये घटनाएँ ‘परिवार को जोड़े रखने वाली’ स्त्री का, पुरुष की ‘टोली-मानसिकता’ का शिकार होने और उसके बुरे परिणाम भुगतने के उदाहरण हैं।
इन घटनाओं के कारणों को समझने के लिए नैसर्गिक मुक्त शारीरिक संबंधों के स्थान पर विवाह के माध्यम से लागू किये गये नियंत्रित शारीरिक संबंध-पद्धति के कारण पुरुष और समाज पर जो परिणाम दिखाई देता है, उसकी भी पड़ताल करनी होगी। परिवार-व्यवस्था में सम्मिलित किये जाने के साथ-साथ पुरुष के नैसर्गिक आक्रामक मूल्यों का उपयोग धीरे-धीरे घटने लगा; जिसके कारण पुरुष में विद्यमान ऊर्जा के उपयोग का सवाल तीव्रता के साथ उभरा। इसके साथ ‘अनेक स्त्रियों के साथ संबंध और मैत्री रखने’ की टोली-जीवन की आदतें और नैसर्गिक अधिकार विवाह के कारण छिन गए। फलस्वरूप पुरुष की नई भिन्न प्रकार की समस्याएँ पैदा होने लगीं। नए वैवाहिक संबंधों में आने वाले इन बदलावों को स्वीकारते हुए, उससे निर्मित होने वाली पुरुष की शारीरिक अड़चनों और मानसिक अवस्था के दुष्परिणामों का अध्ययन कभी नहीं किया गया। इन स्थितियों में पुरुष में आने वाली निराशा और रिक्तता को भरने संबंधी, ‘परिवार के अनुकूल उसका सशक्तीकरण किये जाने संबंधी विचार कभी नहीं किया गया। बल्कि, इस रिक्तता को भरने के लिए, विवाह-बंधन के स्वीकार के कारण जंगली अवस्था में प्राप्त, परंतु अब पुरुष द्वारा खोई गई सार्वभौमिक निरंकुश सत्ता की भरपाई करने का अवसर, उसी विवाह के माध्यम से उसे हासिल हुआ। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि मामलों में परिवार-प्रमुख के स्थान से, उसी विवाह द्वारा कब्जे में आई स्त्री के विरोध में पुरुष को अनायास इस वर्चस्व का अवसर हासिल हुआ। और यहीं से पुरुषप्रधान या पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ। फिर इस तरह पुरुष-केन्द्रित सत्ता पर आसीन पुरुष, मनुष्य के जीवन-संघर्षों में बचाए हुए ‘पारिवारिक मूल्यों’ को मज़बूत करने के लिए, उसमें अपने-आप को ‘अबल’ (असमर्थ) मानकर, खुद के सशक्तीकरण का विचार करे; और वह भी ममता, संयम, संवेदना, सौजन्य जैसे गुणों को अपनाकर, यह बात असंभव मानी गई। मानव-समाज के ‘परिवार-सर्वाइवल’ के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएँ, जिनमें स्त्रियाँ अनेक सदियों से पली-पगी, सम्पन्न हुई थीं, उन पर ‘स्त्रियोचित’ का ठप्पा लगाकर उनका उपहास किया जाने लगा। और पुरुष के प्राचीन अवस्था के आक्रामकता जैसे गुणधर्मों को ही सच्ची ‘मर्दानगी’ घोषित करके स्थापित किया गया।(क्रमशः)