उषा वैरागकर आठले
(मुंबई के अलग अलग उपनगरों में काफी बड़ी संख्या में ऑडिटोरियम हैं। अधिकांश ऑडी में मराठी या गुजराती के कमर्शियल नाटक निरंतर चलते रहते हैं। सभी नाटकों की खोजखबर ‘book my show से मिलती रहती है। इसलिए टिकट बुक करके बहुत आसानी से नाटक देखा जा सकता है। पृथ्वी थिएटर में हिंदी नाटक नियमित होते हैं। वहाँ इंटिमेट थिएटर के कारण नाटक देखने की सार्थकता कुछ और ही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वहाँ के दर्शक प्रायः नाट्यप्रेमी जन ही होते हैं या फिर विभिन्न नाट्य दलों से जुड़े रंगकर्मी; सामान्य दर्शक प्रायः नहीं दिखाई देते, जैसे छोटे शहरों या कस्बों में दिखाई देते हैं।
‘सहयात्री’ की लेखन-यात्रा कुछ दिनों के लिए थोड़ी डाइवर्ट हो गई थी। कुछ दूसरे लेखन कार्यों में संलग्न हो जाने के कारण ब्लॉग-लेखन रूक-सा गया था। अपनी अनुभव-यात्रा का स्वरूप बरकरार रखते हुए इस बीच देखे हुए अनेक हिंदी-मराठी नाटकों पर टिप्पणियों के साथ कुछ कड़ियाँ प्रस्तुत हैं। तीसरी कड़ी है, नसीरुद्दीन शाह निर्देशित नाटक ‘इस्मत आपा के नाम ’। सभी फोटो गूगल से साभार लिए गए हैं। )
9 अप्रेल की शाम दो मायनों में मेरे रंगमंचीय जीवन की बहुत खास शाम थी। पहला, इप्टा की बहुप्रतीक्षित सांस्कृतिक यात्रा ‘ढाई आखर प्रेम’ की शुरुआत रायपुर से हो रही थी, जो पाँच हिंदीभाषी राज्यों – छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश में 9 अप्रेल से 22 मई तक आयोजित की गई थी। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करने तथा चारों तरफ फैलते जा रहे नफरत के धुएँ को प्रेम की शीतल फुहारों से विरल करने की कोशिश में इप्टा के साथी निकल पड़े थे गाँव-शहर के रास्तों से गली-कूचों तक।
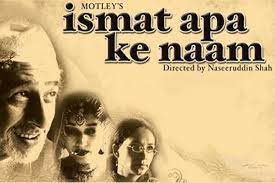
दूसरा, लैंगिक भेदभाव तथा बेहूदे यथार्थ को तुर्शी और व्यंग्य के साथ अद्भुत तरीके से गूँथकर स्तब्ध कर देने वाली कहानियाँ लिखने वाली इस्मत चुगताई की तीन कहानियों का मंचन देखना। मोटले ग्रुप के बैनर पर अभिनय के जादूगर नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह तथा हीबा शाह की प्रस्तुति पृथ्वी थियेटर में बहुत नज़दीक से देखना एक नायाब अनुभव रहा। अपनी समूची देहगतियों, मुख-मुद्राओं, आवाज़ के उतार-चढ़ाव-मौन तथा आँखों की भाषा का सम्प्रेषण इतनी बारीकी से करने वाला अभिनय, बिल्कुल मामूली प्रॉपर्टीज़ के उपयोग की सार्थक रंग-भाषा को एक साथ एक मंच पर देखना अविस्मरणीय था। अभिनय का इस्मत आपा की कहानियों के पात्रों और घटनाओं के साथ इसतरह घुलमिल जाना कि, महसूस होता था कि कहानी की परत-दर-परत प्याज़ के छिलकों की तरह खुलती जा रही है। और यह सबकुछ इतने इत्मीनान और सहज विनोद के साथ किया जा रहा था कि हँसते-खेलते बताई जा रही कथा एक साथ दिल को छलनी किये जा रही थी, पर होठों पर मुस्कुराहट या कभी कभी खिलखिलाहट भी अनायास छूट जाती थी। प्रस्तुति खत्म होने के बाद बार-बार खयाल आ रहा था कि इस्मत चुगताई ने उस ज़माने में जिस बारीकी से पितृसत्तात्मक वर्चस्ववाद के असरात को अपने महिला और पुरुष पात्रों के माध्यम से, घटनाओं से अभिव्यक्त किया है, उसका आज भी कोई सानी नहीं है।

नसीरुद्दीन शाह ने नाटक की शुरुआत में इस्मत चुगताई के प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े होने, कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी जैसे दिग्गज साहित्यकारों के बीच एक महिला साहित्यकार का इसतरह अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी चर्चा करते हुए कहा कि उनकी 1942 में लिखी कहानी ‘लिहाफ’ को लेकर उस समय किसतरह अश्लीलता का आरोप लगाकर मुकदमेबाज़ी हुई मगर कोर्ट में यह आरोप साबित नहीं हो सका, लोग इसकी चर्चा तो करते हैं मगर उनकी अन्य कहानियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि हम ये तीन कहानियाँ सुनाएंगे ज़रूर, मगर आपको वे अपनी आँखों के सामने घटित होते हुए भी दिखेंगी! वाकई वे चरित्र, उनका परिवेश, उनकी गतिविधियों को कहानी-दर-कहानी दर्शकों ने आँखो देखी घटना की तरह जिया।

जिन कहानियों को मंच पर देखा था, उन कहानियों को मैंने घर आकर इंटरनेट पर पढ़ा और मुझे लगा कि इस नाट्य प्रस्तुति के बारे में लिखते हुए मुझे इस्मत चुगताई की कहानी के कुछ अंशों को भी उद्धृत करना चाहिए। क्योंकि इस मंचन में जितना अभिनय और प्रस्तुति का प्रभाव है, लगभग उतना ही कहानी के कथ्य और इस्मत चुगताई की कहन शैली का भी। नाट्य-प्रस्तुति में ‘कहानी का रंगमंच’ की तरह ही एक भी शब्द को छोड़ा नहीं गया था मगर मुझे साफ़ कहना होगा कि ‘कहानी का रंगमंच’ को लोकप्रिय बनाने वाले रंग निर्देशक देवेन्द्रराज अंकुर की प्रस्तुतियों से नसीरुद्दीन शाह के निर्देशन की यह कहन शैली रंगकर्म की गहरी तहों को कहीं ज़्यादा बेहतर संवेदनशीलता और वैचारिकता के साथ बुनती है और ज़्यादा असरदार है। मंच पर सिर्फ एक बड़ा तखत, उस पर दो गावतकिये, पानी की सुराही मौजूद थी। हरेक कहानी के बाद पाँच मिनट में सिर्फ तखत की चादर का बदलना और कुर्सी, लैम्प या फिर हुक्के जैसी एकाध प्रॉपर्टी का सम्मिलित किया जाना भी सादगीभरा था। लाइट कहानी के मूड्स के अनुसार, मगर कहीं भी कथ्य पर हावी नहीं।

शीबा शाह द्वारा प्रस्तुत पहली कहानी थी ‘छुईमुई’। कहानी की शुरुआत ही दिलचस्प तरीके से होती है, ‘‘आराम कुर्सी रेल के डिब्बे से लगा दी गई और भाई जान ने क़दम उठाया, ‘इलाही ख़ैर… या ग़ुलाम दस्तगीर… बारह इमामों का सदक़ा। बिसमिल्लाह बिसमिल्लाह… बेटी जान सँभल के…क़दम थाम के…पांयचा उठाके… सहज सहज।’ बी मुगलानी नक़ीब की तरह ललकारीं। कुछ मैंने घसीटा’, कुछ भाई साहब ने ठेला। तावीज़ों और इमामज़ामिनों का इश्तहार बनी भाभीजान तने हुए गुब्बारे की तरह हाँपती सीट पर लुढ़क बैठीं।’’ एक फूलों की तरह पली-बढ़ी लड़की शादी के बाद भी उतने ही नाज़-नखरे-आराम के साथ रहते हुए अगले साल ही गर्भवती होती है मगर लगातार दो बार वह खाली हाथ हो जाती है। तीसरी बार काफी ध्यान-जतन के बाद दिल्ली से अलीगढ़ जचकी के लिए तूफान मेल से ले जाई जाती है, उस यात्रा का समूचा वर्णन कहानी में गजब की दृश्यात्मकता के साथ किया गया है। आगे चलकर गाजियाबाद स्टेशन पर एक गरीब गर्भवती औरत अचानक चढ़ती है और देखते-देखते उसको बच्चा भी वहीं हो जाता है। उसका पूरा वर्णन, उस गरीब औरत का सहजता के साथ खुद ही बच्चे को साफ करना, उसकी नाल काटना, खुद को और डिब्बे को साफ कर मुस्कुराते हुए ऊँघने लगना – अमीरी और शानोशौकत में पली-बढ़ी बी मुगलानी और किशोरी ननद के साथ भाभी जान को बुरी तरह आतंक से भर देता है। अनगिनत मेहनतकश औरतें, जिनको कभी किसी मौके पर आराम या सुख-सुविधा मयस्सर न होती हो, उनके द्वारा बच्चा पैदा करना भी सहज प्राकृतिक क्रिया की तरह घट जाता है। इस्मत चुगताई ने किस गहरे अहसासात के साथ लिखा है, ‘‘उसकी उम्र मेरे जितनी होगी या शायद साल-छः महीने बड़ी हो। वो अपने अल्हड़, ना तजुर्बेकार हाथों से एक बच्चे की नाल काट रही थी जो उसने चंद मिनट पेशतर जना था। उसे देखकर मुझे वो भेड़-बकरियाँ याद आने लगीं जो बगैर दाई और लेडी डॉक्टर की मदद के घास चरते चरते पेड़ तले जच्चाख़ाना रमा लेती हैं और नौज़ाईदा को चाट-चाटकर क़िस्सा ख़त्म करती हैं।’’

समाज में व्याप्त विषमता और वर्गों के बीच की गहरी खाई के दोनों ओर घटते दो अनुभव-संसार तथा महिला-जीवन के अंतर्विरोध चार पात्रों के माध्यम से शीबा शाह ने बखूबी उभारे। सिर्फ एक गाव तकिया, डायरी, पेन और चश्मे के साथ बड़े से तख्त पर अकेले ही अनेक गतिविधियाँ करते हुए कहानी को एक झटके से खत्म किया।
दूसरी कहानी ‘मुगल बच्चा’ रत्ना पाठक शाह ने अपनी नायाब शैली में इस तरह सुनाई कि लगा, कोई दादी अपने नाती-पोतों के पूरे कुनबे को सामने बैठाकर कहानी कहती जा रही हैं। एक ऐसी दादी, जो मक्खन की तरह कोमल और गोरी चिकनी खूबसूरती की मूरत हुआ करती थीं। कई बच्चों के मरने के बाद पैदा हुईं थीं इसलिए बहुत नाज़-नखरों से पाली हुई! मगर बारह-तेरह की हुई नहीं कि ब्याह दी गईं एक ऐसे नवाब को, जो एकदम काले कोयले जैसा था। हँसी-मज़ाक में हमेशा ही परिवारजन और दोस्त-सहेलियाँ दूल्हे-दुल्हन को चिढ़ाते-चढ़ाते रहते हैं, वैसा ही वाकया दोनों के साथ होता है। कोई दुल्हन को समझाइश देती है कि शरमाती लजाती रहना, मगर अपने हाथ से अपना घूँघट मत उठाना! वहीं दूल्हा तो ठहरा नवाबज़ादा! ‘‘मैं मर जाऊँगा, पर कसम नहीं तोडूँगा’ कहावत को चरितार्थ करती चुग़ताई खानदान के एक फ़र्द की कहानी है यह। वह काला भुजंग है, लेकिन उसकी शादी उतनी ही गोरी लड़की से हो जाती है। एक काले ‘मुग़ल बच्चे’ की गोरी दुल्हन से शादी होने पर लोग उसका मज़ाक़ उड़ाते हैं और उसे ताने देते हैं। इन सबसे तंग आकर वह ऐसी कसम खाता है जिससे उसकी और उसकी गोरी दुल्हन की शादीशुदा ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। वह सोचकर ही कमरे में प्रवेश करता है, ‘‘ब’ख़ुदा में इसका ग़रूर चकनाचूर कर दूँगा। किसी ऐसे वैसे से नहीं, मुग़ल बच्चे से वास्ता है।’’

रत्ना पाठक शाह ने उस रात के संवादों को कुछ इसतरह की कहन में सुनाया कि समूची तस्वीर आँखों के सामने खड़ी हो गई। इस्मत चुग़ताई की ग़ज़ब की कहन शैली तो बेमिसाल है ही। सामाजिक रीतिरिवाज़ों की विसंगतियों का कच्चा चिट्ठा वे जिस मज़ाकिया अंदाज़ में खोलती हैं, उसे रत्ना जी ने बड़ी बारीक़ी से प्रस्तुत किया,
‘‘काले मियां फुंकारे काले मियां शहतीर की तरह पूरी मसहरी पर दराज़ थे। दुल्हन एक कोने में गठरी बनी काँप रही थी। बारह बरस की बच्ची की बिसात ही क्या!
‘‘घूँगट उठाओ।’’ काले मियां डकराए
दुल्हन और गड़ी मुड़ी हो गई।
‘‘हम कहते हैं घूँगट उठाओ।’’ कोहनी के बल उठकर बोले।
सहेलियों ने तो कहा था। दूल्हा हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा पर ख़बरदार जो घूँगट को हाथ लगाने दिया। दुल्हन जितनी ज़्यादा मुदाफ़’अत करे, उतनी ही ज़्यादा पाक-बाज़।
‘‘देखो जी, नवाबज़ादी होगी अपने घर की, हमारी तो पैर की जूती हो। घूँगट उठाओ। हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं।’’
दुल्हन पर जैसे फ़ालिज गिर गया।
काले मियां चीते की तरह लपक कर उठे, जूतियाँ बग़ल में दाबीं और खिड़की से पाइँबाग़ में कूद गए। सुबह की गाड़ी से वो जोधपुर दनदना गए।’’ वहाँ जाकर वे घुड़सवारों में भर्ती हो गए।
यह किस्सा शादी की पहली रात का है। गोरी दादी कुँवारी रह जाती हैं। दोनों खानदानों में इस बात पर तलवारें खिंच जाती हैं। मगर होता कुछ नहीं। कुछ सालों के बाद काले मियाँ को बावा के बीमारी की ख़बर देकर बुलवाया जाता है। वे आते हैं, फिर उनकी गृहस्थी बसाने की कोशिश की जाती है। ‘मगर शर्त वही रही कि हश्र हो जाए मगर घूँगट तो दुल्हन को अपने हाथों उठाना पड़ेगा। ‘‘क़िबला कअ’बा मैं क़सम खा चुका हूँ। मेरा सर क़लम कर दीजिए, मगर क़सम नहीं तोड़ सकता।’’
‘‘ख़ैर साहब, गोरी बी फिर दुल्हन बनाई गईं। … अम्मां ने समझाया। ‘‘तुम उसकी मनकूहा हो बेटी जान। घूँगट उठाने में कोई ऐब नहीं। उसकी ज़िद पूरी कर दो, मुग़ल बच्चा की आन रह जाएगी। तुम्हारी दुनिया सँवर जाएगी, गोदी में फूल बरसेंगे। अल्लाह रसूल का हुक्म पूरा होगा।’’ मगर हाय रे किस्मत! वाकया ये हुआ…
‘‘घूँगट उठाओ।’’ काले मियाँ ने बड़ी लहाज़त से कहना चाहा मगर मुग़ली दबदबा ग़ालिब आ गया।
गोरी बेगम ग़ुरुर से तमतमाई सन्नाटे में बैठी रहीं।
‘‘आख़िरी बार हुक्म देता हूँ। घूँगट उठा दो, वर्ना इसी तरह पड़ी सड़ जाओगी। अब जो गया, फिर ना आऊँगा।’’
मारे ग़ुस्से के गोरी बी लाल भबूका हो गईं। काश उनके सुलगते रुख़्सार से एक शोला लपकता और वो मनहूस घूँगट ख़ाक हो जाता।
बीच कमरे में खड़े काले मियाँ कौड़ियले साँप की तरह झूमते रहे। फिर जूते बगल में दबाए और पाइंबाग़ में उतर गए।’’

इसके बाद चालीस बरस बीत गए। गोरी बी के गहने एक-एक कर लालाजी की तिजोरी में पहुँच गए। लेकिन अचानक एक दिन ‘‘काले मियाँ आप ही आन धमके। उन्हें क़िस्म क़िस्म के ला-इलाज अमराज़ लाहक़ थे। पोर पोर सड़ रही थी। रोम रोम रिस रहा था। बदबू के मारे नाक सड़ी जाती थी। बस आँखों में हसरतें जाग रही थीं, जिनके सहारे जान सीने में अटकी हुई थी। ‘‘गोरी बी से कहो मुश्किल आसान कर जाएँ।’’
कहानी के क्लाइमैक्स पर रत्ना जी की किस्सागोई ने दर्शकों की जिज्ञासा को चरम पर पहुँचा दिया था। वे मानों अपनी आँखों देखी हम सबको सुना रही थीं और हम सब देखते चले जा रहे थे।
‘‘एक कम साठ की दुल्हन ने रूठे हुए दूल्हे मियाँ को मनाने की तैयारियाँ शुरु कर दीं। मेहँदी घोलकर हाथ पैरों में रचाई। पानी समो कर पंडा पाक किया। सुहाग का चकटा हुआ तेल सफ़ेद लटों में बसाया। संदूक़ खोलकर बोर बोर टपकता झड़ता बरी का जोड़ा निकालकर पहना और इधर काले मियाँ दम तोड़ते रहे।
जब गोरी बी शरमाती लजाती धीरे धीरे क़दम उठाती उनके सिरहाने पहुँची, तो झंगे पर चीकट तकिये और गोडर बिस्तर पर पड़े हुए काले मियाँ की मुट्ठी भर हड्डियों में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। मौत के फ़रिश्ते से उलझते हुए काले मियाँ ने हुक्म दिया, ‘‘गोरी बी, घूँगट उठाओ।’’
गोरी बी के हाथ उठे मगर घूँगट तक पहुँचने से पहले ही गिर गए।
काले मियाँ दम तोड़ चुके थे।
वो बड़े सुकून से उकडॅूँ बैठ गईं, सुहाग की चूड़ियाँ ठंडी कीं और रंडापे का सफ़ेद आँचल माथे पर खिंच गया।’’
यहाँ कहानी समाप्त होती है और धीरे धीरे लाइट फेड आउट होती है अगली कहानी के लिए। मैंने इस्मत चुगताई की यह कहानी नहीं पढ़ी थी। एक औरत की ज़िंदगी का शादी और घर-गृहस्थी के इर्दगिर्द बुना हुआ सुख-दुख का तानाबाना उसे किस हद तक एक मज़ाक बना देता है! खासकर उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की औरत! उसका व्यक्तित्व, उसका स्वाभिमान, उसका वजूद… ये किस चिड़िया का नाम है!!! इस अहसास से ऑडिटोरियम में शायद सभी डूब-उतरा रहे थे… शायद पाँच मिनट के लिए … तभी लाइट जलती है और दिखाई देते हैं नसीरुद्दीन शाह कहानी ‘घरवाली’ कहने के लिए तैयार!

कहानी में इस्मत चुगताई औरत की ओर देखने की बहुत ही घटिया मर्दवादी दृष्टि को बारीक तुर्शी मगर हास्य-विनोद वाली शैली में बयाँ करती हैं। औरत-मर्द संबंधों के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक पहलुओं का कच्चा चिट्ठा वे बहुत खुलकर प्रस्तुत करती हैं। इस्मत आपा के निहित उद्देश्य को अपनी सूक्ष्म अभिनय क्षमता के साथ नसीरुद्दीन जिसतरह प्रस्तुत करते हैं, उसमें खुले हुए फूहड़ संदर्भ भी फूहड़ नहीं लगते, बल्कि सामाजिक मर्दवादी वर्चस्व की बखिया उधेड़ते हुए लगते हैं। एक पुरुष अभिनेता द्वारा समाज में स्त्री की ओर देखने का अत्यंत संकुचित, उपभोगवादी, अनैतिक और तकलीफदेह नज़रिया जिस संवेदनशीलता के साथ वे उभारते हैं, वह काफी सुखद मालूम देता है।

कहानी प्रमुख रूप से दो पात्रों के बीच घूमती है – कुँवारे अधेड़ मिर्ज़ा और सड़कों पर बिना घरबार की पली-बढ़ी बला की खूबसूरत लाजो के बीच। लाजो का विवरण इस प्रकार है, ‘‘पता नहीं किस अरमानभरी ने लाजो का नाम रखा होगा! लाज और शरम का तो लाजो की दुनिया में कोई मतलब न था!’’ समाज में भूखी नज़रों के बीच पली बढ़ी अनाथ बच्ची और किसतरह की युवती बन सकती थी भला! मिर्ज़ा के नौकर के भाग जाने के बाद मिर्ज़ा के एक दोस्त लाजो को उनके घर छोड़ जाते हैं, जिसका उपभोग वे कर चुके हैं। मिर्ज़ा अविवाहित होने के बावजूद औरतबाज़ व्यक्ति थे मगर वे अपने घर में लाजो जैसी औरत को काम के लिए रखने के नाम पर भी तुनककर कहते हैं, ‘‘लाहौल बिल्लाकुव्वत! मैं नीच औरतों को घर में डालने का कायल नहीं।’’ बावजूद इसके लाजो उनकी बात को नज़रअंदाज़ कर उनके घर में घुसते ही घर के कामकाज में ऐसे लग जाती है, मानो उसी का घर हो। शाम को जब मिर्ज़ा घर आते हैं, उन्हें अपना ही घर पहचान में नहीं आता। इतना साफ़शफ्फ़ाक़! इतना स्वादिष्ट खाना! मगर मिर्ज़ा उसे वापस छोड़कर आने की बात कहते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे उसकी तनख्वाह दे सकें। इस पर लाजो बात समाप्त करते हुए कहती है कि उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि ‘‘पहली ही नज़र में लाजो दिल दे बैठी थी। मिर्ज़ा को नहीं, घर को। बगैर मालकिन का घर अपना ही हुआ न! घर मर्द का थोड़े ही होता है, वो तो मेहमान होता है!’’

बहरहाल, लाजो मिर्ज़ा के घर का कामकाज संभाल लेती है। बस उसे एक बात का मलाल है कि उसके रहते मिर्ज़ा कंजरियों के पास क्यों जाते हैं! मगर उसका यह मलाल भी दूर होता है और उसके बाद मिर्ज़ा को वह अपनी ‘चीज़’ लगने लगती है। मिर्ज़ा को लाजो का जिस-तिसके मुँह लगना, हँसी-मज़ाक करना कतई नहीं सुहाता और इस पर स्थायी उपाय के रूप में वे लाजो से निकाह पढ़ लेते हैं। लाजो को इसकी ज़रूरत समझ में नहीं आती। वह अपने तईं निकाह का विरोध भी करती है। निकाह के तुरंत बाद लाजो के लिए तंग मुहरी के दो पायजामे-कुर्तियाँ सिलवाई जाती हैं, जिससे लाजो बहुत परेशान होती है। उसे खुले पैरों का लहँगा पहनने की आदत! इस्मत चुगताई कहानी में अनेक स्थानों पर बहुत खुली भाषा में इसतरह की जेंडरवादी पाबंदियों को भदेस परंतु मार्मिक तरीके से व्यक्त करती हैं, उससे एक ओर तो उनके खुलेपन से सुननेवाला चौंकता है पर वहीं दूसरी ओर एक औरत के प्रति ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति’ की तरह देखने का पुरुषवादी नज़रिया एक ज़बर्दस्त प्रतिरोध के रूप में दर्शक को झकझोर जाता है।

नसीरूद्दीन शाह का समूचा नरेशन और आंगिक-वाचिक अभिनय इस्मत के इस प्रतिरोध को शत-प्रतिशत दर्शकों को सम्प्रेषित करता है। निकाह के बाद मिर्ज़ा ‘घरवाली’ के प्रति फिर उदासीन होने लगते हैं और उनके कंजरियों के चक्कर शुरु हो जाते हैं। लाजो को यह बात नागवार गुज़रती है। अब तक आसपास के तमाम पुरुषों के आकर्षण का केन्द्र रही लाजो कोठे के ऊपर पतंग उड़ाने वाले मिठुआ को ढील दे देती है और एक दिन मिर्ज़ा द्वारा रंगे हाथों पकड़ी जाती है। मिर्ज़ा, जिन्होंने उसे अब तक फूल की छड़ी से तक न छुआ था, उसकी लात-घूँसों से मरम्मत करते हैं और अंततः उसे 32 रूपये मेहर के ऐवज में तलाक़ दे देते हैं। ‘‘लाजो को जब तलाक की खबर पहुँची तो जान में जान आई, जैसे सिर से बोझ उतर गया हो। निकाह तो उसे वैसे भी रास नहीं आया था। ये सब इसी मारे हुआ। चलो, पाप कटा!’’ रामू की दादी के घर पंद्रह दिन रहते हुए वह फिर पहले जैसी स्वस्थ हो गई, मानो धूल झाड़कर खड़ी हो गई हो! इस बीच मिर्ज़ा को उसके दोस्तों द्वारा बताया जाता है कि उसका निकाह कोई मायने नहीं रखता क्योंकि नाजायज़ औलाद से निकाह नहीं हो सकता इसलिए निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक के लिए गम कैसा? 32 रूपये बेवजह खर्च हो गए! पर मिर्ज़ा की नाक नहीं कटी! उनके सिर से बोझ उतर गया। पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई। जब लाजो ने यह खुशखबर सुनी, उसका मन खुशी से नाच उठा। ‘‘निकाह और तलाक़ एक बुरा ख़्वाब था, जो खत्म हुआ और जान छूटी। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की थी कि मिर्ज़ा की नाक नहीं कटी। उसे मिर्ज़ा की इज़्ज़त जाने का बड़ा दुख होता। हरामी होना कैसा वक्त पर काम आया!’’ उसे मिर्ज़ा की चिंता सताने लगी कि उसके घर में कूड़े के अंबार लग गए होंगे। एक दिन उसने दुकान जाते मिर्ज़ा का रास्ता रोककर पूछ ही लिया, ‘‘मियाँ, कल से काम पर आ जाऊँ?’’ पहले तो मिर्ज़ा कन्नी काट गए मगर बाद में सोचा कि कोई नौकरानी तो रखनी ही होगी तो यही बदजात ही सही! लाजो ने इंतज़ार नहीं किया। वह छत से कूदकर मिर्ज़ा के घर में पहुँच गई। ‘‘लहँगे का लंगोट किया और काम में जुट गई।’’ मिर्ज़ा शाम को घर पहुँचे तब घर पहले जैसा साफसुथरा महक रहा था। रात को सोचने लगे, ‘‘बड़ी बेकदरी की थी उन्होंने उसकी! लाहौल बिलाकुव्वत! यकायक वो भन्नाए हुए उठे और टाट के पर्दे हटाकर बावर्चीखाने में जाकर ‘घरवाली’ को समेट लिया।’’ कहानी यहाँ खत्म होती है। मिर्ज़ा की कश्मकश, अनाथ आवारा लाजो की आज़ादी, समाज के जेंडरगत दोहरे मापदंड, धर्मों का पाखंड, पुरुष का वर्चस्ववादी चरित्र – नसीरूद्दीन शाह ने बहुत गहरी वैचारिक और अभिनय की समझ से इस्मत चुगताई के पात्रों को मंच पर साकार कर दिया। कुछ दृश्यों में ऐसा लगा कि इस्मत आपा ही सामने आकर कहानी सुना रही हों!

नसीरूद्दीन शाह के निर्देशन में तीनों कहानियों के माध्यम से मर्दवादी समाज में औरत की ज़िंदगी के रेशे रेशे मंच पर खुलते गए। अश्लीलता का आरोप झेलनेवाली इस्मत चुगताई द्वारा समाज के दोगले अश्लील यथार्थ को इसतरह प्रस्तुत किया जाना बीसवीं सदी के चौथे-पाँचवें दशक को कहाँ पच सकता था! हालाँकि आज का यथार्थ तो और भी भयानक हो उठा है। ऐसे माहौल में नसीरूद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और शीबा शाह द्वारा इन कहानियों की बेबाक मगर दिल-दिमाग को हिला देने वाली प्रस्तुति देखना अविस्मरणीय अनुभव रहा।



