(लॉकडाउन के दौरान यूँ ही खोजते-खोजते यूट्यूब पर मुझे कुछ मराठी लघु फ़िल्में मिलीं। जिस तरह मराठी में दलित आत्मकथाओं ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति-व्यवस्था के एक अंधियारे पक्ष को साहित्य के माध्यम से उजागर किया था, जिससे वर्ण-व्यवस्था के क्रूर चेहरे की अनेक मुख-मुद्राओं से पाठकों को रू-ब-रू होने का अवसर मिला, उसी तरह इन लघु फिल्मों ने महाराष्ट्र की अनेक दबी-कुचली-पिछड़ी-वंचित जातियों के जीवन-संघर्ष, विपरीत परिस्थितियाँ, अन्याय, अपमान और उपेक्षा के बावजूद आत्मसम्मान के नए क्षितिज छूने का विशाल संसार मेरे सामने खोल दिया। चूँकि मैं मराठी से हिंदी अनुवाद के माध्यम से मराठी-हिंदी के बीच पुल का काम करती ही हूँ, इसलिए इस काम को थोड़ा विस्तार देते हुए मराठी की इन लघु फिल्मों से परिचय की कुछ कड़ियाँ साझा कर रही हूँ। दूसरी कड़ी में है – लघु फिल्म बलुतं ।)
‘बलुतं’ प्राचीन महाराष्ट्र के गाँवों में रहने वाली बगैर खेती-बाड़ी के वंशानुगत कारीगरी के व्यवसाय करने वाली अछूत तथा पिछड़ी जातियों की सेवा-प्रणाली है। पहले वस्तु-विनिमय के ज़माने में किसान केंद्र में होता था। किसान अन्न उपजाता और जो गैरकिसानी काम करते, वे इनकी तथा अन्य लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे। इन्हें ‘बलुतेदार’ कहा जाता था तथा ये गाँव के ‘वतनदार’ कहलाते थे। इन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी वही काम करना होता था। मराठी विकिपीडिया के अनुसार इनकी संख्या बारह है – कुम्हार, गुरव (मंदिर की साफसफाई करनेवाला), मछुआरा, चमार, मातंग, तेली, नाई, धोबी, माली, महार, लुहार तथा बढ़ई। वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनेवाले मराठी के अद्भुत साहित्यकार अण्णाभाऊ साठे के कथा-साहित्य में महाराष्ट्र के कोने-अंतरे में जीवनयापन करनेवाली अनेक उपेक्षित-वंचित जातियों के पात्रों एवं उनकी विषम परिस्थिति की सूक्ष्म अभिव्यक्ति मिलती है। प्रस्तुत फिल्म नाई जाति की एक विधवा स्त्री के साहस और स्वाभिमान के विजय की सत्यकथा पर आधारित फिल्म है।
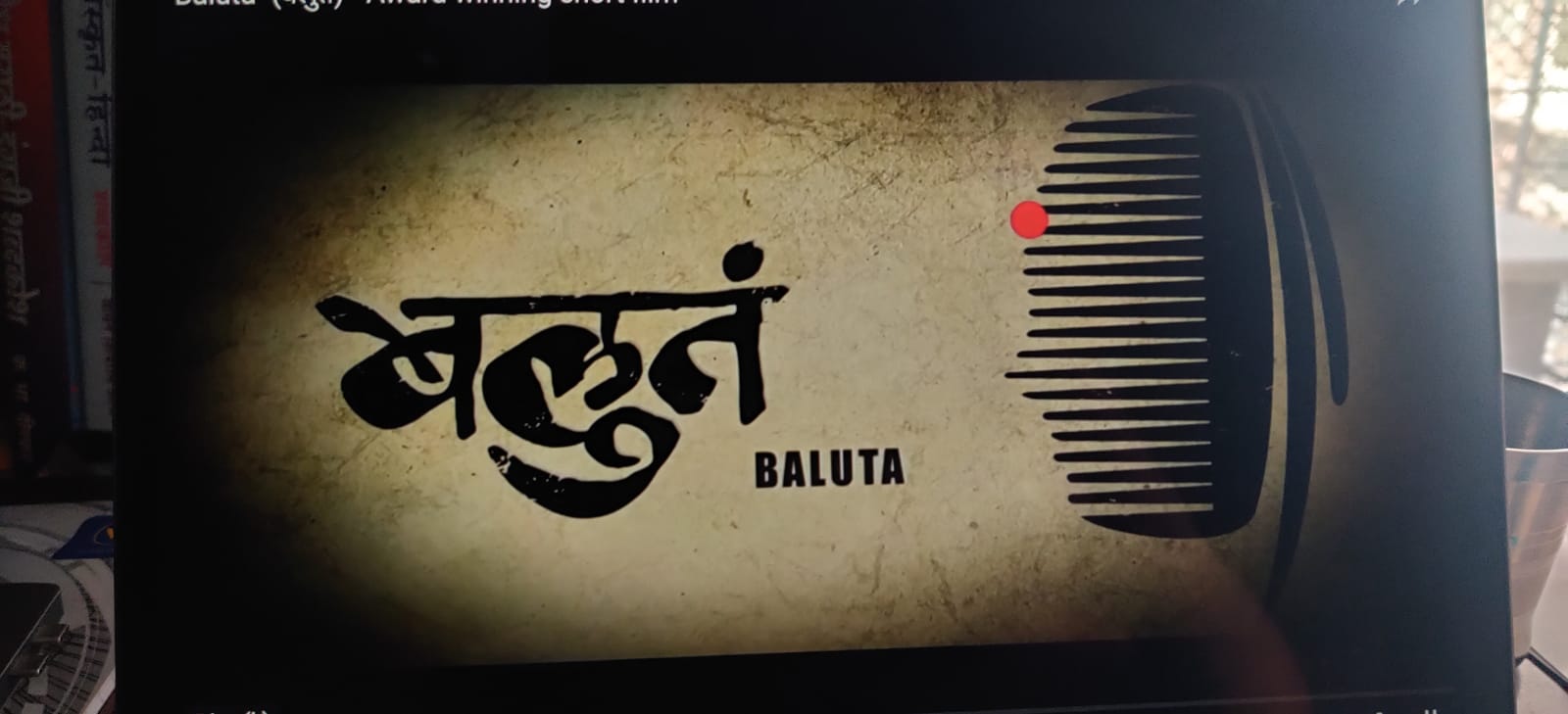
भारत गाँवों का देश कहा जाता है। कुछ दशकों पहले तक बड़े पर्दे पर देश के विभिन्न गाँवों का जीवन और कथाएँ दिखती थीं। मगर पिछले तीन-चार दशकों से बड़े पर्दे के साथ-साथ छोटे पर्दे से भी गाँव गायब होता चला गया। हालाँकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से यूट्यूब के अलावा ओटीटी के विभिन्न मंचों पर अब फिर से कुछ ज़मीनी फिल्में देखी जा सकती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह बात बहुत उल्लेखनीय है कि मराठी की अनेक लघु फिल्में ग्रामीण समाज की तलछट माने जाने वाले लोगों के जीवन-संग्राम के यथार्थ चित्र उकेर रही हैं।इनके निर्माता-निर्देशक प्रायः कोई नामीगिरामी लोग नहीं हैं, मगर उनकी ‘कैमरे की आँख’ जिस सूक्ष्मता से समाज के तानेबाने को उजागर करती है, वह काबिलेतारीफ़ है।
निखिल छुरी निर्मित अजय कुराने निर्देशित मराठी लघु फिल्म ‘बलुतं’ में स्वप्निल राजशेखर की पटकथा की शुरुआत काफी क्रांतिकारी लहज़े से होती है। गाँव के बाहर शव-दहन की तैयारी है और एक महिला की हल्की पुकार सुनाई देती है – ‘शांता…!’ शांता मुड़कर देखती है। कुछ औरतें खड़ी हैं, वे शांता को संकेत करती हैं। शांता के पति का अंतिम संस्कार होने वाला है। गाँववाले शांता के देवर को चिता में अग्नि देने के लिए बुलाते हैं मगर अग्नि देने का पलीता आगे बढ़कर शांता थाम लेती है। सभी मर्द एकदूसरे की ओर देखते हैं। शांता के देवर की मूक सम्मति के बाद शांता अपनी बेटी के साथ पति की चिता को अग्नि देती है।

दूसरे दृश्य में शांता जंगल में लकड़ियाँ बीनती हुई दिखती है। देवर वहाँ उसे बताने आया है कि भाई के बाद भाई का ‘नाई का काम’ अब गाँव में वह सम्हालेगा, पंचायत में उसने सूचना दे दी है इसलिए बाल काटने के भाई के औज़ार कल लेने आएगा। दोनों भाइयों में झगड़ा था। शांता उसे ताना मारती है कि भाई के रोज़गार में हिस्सा बँटाने तो आ गए मगर अब तक भाभी और उसकी चार बच्चियों की कोई सुध तक उसने नहीं ली।

तीसरे दृश्य में शांता बाल काटने के पति के औज़ार खोलती है, जो उसके घर की दाल-रोटी चलाते थे। औज़ार देखते हुए उसे अपना बचपन याद आता है, जब वह अपने पिता के साथ काम पर जाया करती थी। पिता कभी उसे चिढ़ाते हैं कि ‘आ, तू भी बाल काट…’ वह हँस देती थी मगर पिता का काम ध्यान से देखती रहती थी। औज़ार देखकर उसके मन में बिजली कौंधती है कि क्यों न वह अपने पति का काम खुद ही सम्हाल ले! वह कैंची हाथ में लेकर चलाकर देखती है। उसमें कुछ आत्मविश्वास आता है। वह अपनी बेटी को मनाते हुए उसके बाल काटती है। अपने काम से संतुष्ट होकर दूसरे दिन वह अपनी बेटी के साथ पति के लिए गाँव द्वारा निर्धारित नाई काम के स्थान पर जाती है। एक छप्पर के नीचे कुर्सी, आईना रखने की पटिया आदि पड़े हुए है। शांता और उसकी बेटी साफ-सफाई करती हैं, आईना दीवार से लगी पटिया पर रखती हैं, सब औज़ार और सामान निकालकर रखती हैं। नारियल फोड़कर पूजा करती हैं। दीवार पर टंगी हुई कबीर के साथी संत सेना, जो इसी नाई जाति के थे, की तस्वीर भी ध्यान खींचती है।

छप्पर के सामने बैठे तीन मर्द देख रहे हैं। एक आकर पूछता है कि ‘‘क्या दुकान शुरु कर रहे हैं? मगर शिरपा का भाई कहाँ है?’’ शांता आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, ‘‘मैं ही काम शुरु कर रही हूँ।’’ वह उसका मज़ाक उड़ाता चला जाता है। दो-तीन दिन माँ-बेटी ग्राहक के इंतज़ार में बैठी रहती हैं, कोई ग्राहक नहीं आता। शाम को वे सामान समेटकर घर लौट जाती हैं। गाँव में खुसुरपुसुर होने लगती है। सरपंच की पत्नी शांता को समझाइश देती है कि कहीं न कहीं रोजी-मजूरी उसे मिल ही जाएगी। क्यों वह नियम-परम्पराओं को तोड़कर गाँव को थूकने का अवसर दे रही है!
शांता के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरे दिन जब वे छप्पर के नीचे बैठी हैं, एक ग्राहक आता है, पूछता है ‘‘कारीगर कहाँ है?’’ शांता कहती है – ‘‘मैं ही हूँ।’’ वह हड़बड़ा जाता है और उसे मना करते हुए भाग जाता है। उसी समय उसकी छोटी बेटी पुकारते हुए आती है कि घर में ग्राहक आया है। माँ-बेटी खुश होकर सभी औज़ार आदि समेटते हुए घर की ओर दौड़ पड़ती हैं। देखती हैं तो एक औरत अपनी भैंस को लेकर आई है, कहती है कि ‘‘घर के मर्द तो आने से रहे, भैंस के ही बाल साफ कर दे!’’ शांता एक मिनट सोचती है मगर घर आए ग्राहक को न ठुकराकर भैंस के बाल साफ करने लगती है।

दृश्य संवेदनशील दर्शक के रोंगटे खड़े कर देता है। वह औरत उसको प्रशंसा भाव से देखते हुए कहती है, ‘शेरनी है तू!’ हाथ पर रखे पैसे देखती है शांता… पहली कमाई के पैसे! (औरत औरत की दुश्मन नहीं होती, जो कि बहुप्रचलित मान्यता है। मैंने इस दृश्य को मन ही मन सलाम किया।)
शांता का देवर सरपंच से शिकायत करता है। सरपंच दोनों को बुलाकर समझाते हैं। कुछ गाँववाले भी हैं। शिरपा उस छोटे से गाँव का इकलौता नाई था। सरपंच कहते हैं – ‘‘पूरा गाँव फँसा पड़ा है, दाढ़ी बनवाने के लिए भी तहसील जाना पड़ता है। और तुमने अलग तमाशा मचा रखा है! क्या कभी किसी औरत के हाथ में उस्तरा देखा है? कौनसा पुरुष तुमसे बाल कटवाएगा? बस करो, अब तुम्हारा देवर ये काम करेगा।’’ देवर को शह मिल जाती है। वह अपनी भाभी के खिलाफ फूहड़ बातें करने लगता है। शांता शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ती है, उसे चुप कराती है और सरपंच से कहती है, ‘‘चार बच्चियाँ हैं मेरी गोद में। अब तक न तो मैंने किसी के सामने हाथ फैलाया है और न चोरीचपाटी की है। मैं मेहनत करूँगी। घर का पुश्तैनी धंधा है। ईमानदारी से करूँगी। आप पढ़े-लिखे हैं। मैं नहीं जानती, औरत को क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं; पता नहीं किस शास्त्र में क्या लिखा है! मगर इतना जानती हूँ कि मेहनत करने वाले को भगवान भी सहारा देते हैं।’’ वह सरपंच को प्रणाम कर लौट जाती है।

दूसरे दिन फिर वह छप्पर के नीचे दुकान सजाती है। अचानक सरपंच आते हुए दिखाई देते हैं। माँ-बेटी आतंकित हो जाती हैं। मगर सरपंच अपनी पगड़ी उतारकर उसके हाथ में देते हैं और खुद कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। शांता बहुत उत्साह से उन्हें कपड़ा ओढ़ाती है और बालों में पानी लगाकर एकाग्रता के साथ उनके बाल काटने लगती है किसी कुशल नाई की तरह;

सरपंच उसका काम देखकर मुस्कुराते हैं। उठते हैं, पटिये पर उसका मेहनताना रखते हैं। तब तक तमाशबीनों की भीड़ लग जाती है। सरपंच घोषणा करते हैं – ‘‘शांता इस गाँव की बेटी है और इस गाँव की ‘बलुतेदार’ भी। रीतिरिवाज़ के अनुसार इसके पति को जो कुछ दिया जाता था, वह सब अब शांता को मिलेगा।’’ वे दूसरे आदमी को भी दाढ़ी बनवाने के लिए बैठने का निर्देश देते हैं।(काश! इसतरह की समझ सभी मर्दों में विकसित हो!) साथ ही सरपंच के पीछे दिखने वाली जाँत-पाँत का विरोध कर मानव-समानता के लिए कबीर, रैदास, पीपा के साथ सत्संग लगाने वाले संत सेना की तस्वीर सार्थक लगने लगती है।

शुरू में ही निर्माता-निर्देशक स्पष्ट करते हैं कि यह फिल्म एक सत्य घटना से प्रेरित एक सृजनात्मक कलाकृति है। कहानी समाप्त होने पर शांताबाई यादव की बाल काटती हुई तस्वीर के साथ हम स्क्रीन पर लिखा हुआ पढ़ते हैं –
‘‘40 साल पहले, शांताबाई यादव ने सभी रूढ़ि-परम्पराओं को तोड़कर निर्णय लिया कि वह अपने नाई पति के धंधे को ही अपनी रोजी-रोटी का साधन बनाकर अपनी बेटियों का पालन-पोषण करेगी। उस समय उसे ‘स्त्री-मुक्ति’ के बारे में कुछ भी पता नहीं था मगर उसके द्वारा लिया गया निर्णय निश्चित ही ‘स्त्री-सशक्तीकरण’ की दिशा में एक मजबूत कदम था। उसकी इस यात्रा में उसके साथ हसूर, गांधिलगंज के गाँववाले थे। आइये, अपने परिवार और धंधे के प्रति शांताबाई के साहस और समर्पण को हम सलाम करें।’’ (मैंने शांताबाई के साथ-साथ फिल्म के निर्माता-निर्देशक को भी सलाम किया।)

बहुत छोटे-छोटे दृश्यों में गरीबी, असहायता से उपजी समझदारी, बच्ची के चेहरे के भाव और बातचीत सीधे दिल पर चोट करती है। एक दृश्य में लकड़ी लाने के बदले मिला थोड़ा चावल पकाकर माँ-बेटी खा रहे हैं। आधा खाने के बाद बेटी पानी की देगची उठाकर पीने लगती है। माँ अपनी तरल आँखों से कहती है, ‘पेट भर पी ले!’ संवाद छोटा-सा है, मगर उसकी आँखों के भाव बहुत-कुछ कह जाते हैं। रात को सोने से पहले बच्ची माँ से कहती है, ‘‘मैं अगर लड़का होती तो बापू के काम को सम्हाल लेती, फिर हमें पेट भर खाने को मिल जाता!’’ नाई काम सिर्फ पुरुष द्वारा किये जाने का गहरा अफसोस उसकी आवाज़ में उभरता है। अन्य दृश्य में जंगल में कुआँ देखकर शांता उसमें कूदकर परेशानियों से निजात पाने की बात सोचकर कदम बढ़ाती है, तभी उसकी बेटी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर आते हुए पुकारती है। शांता होश में आती है। बेटी को देखती रहती है फिर उसका हाथ मजबूती से थाम लेती है। अपनी बेटियों के लिए जीने का संकल्प उसे मजबूती देता है।
एक स्वाभिमानी स्त्री के दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास को देखकर सरपंच द्वारा स्वयं प्रोत्साहन देना अवश्य फैंटेसी लगता है, मगर गाँव की अधिकांश औरतों का उससे सहानुभूति रखना, उसका साथ देना भी सकारात्मक प्रेरणा देता है।फिल्म में स्त्री-पुरुष के स्टीरिओटाइप्ड छवियों को तोड़कर जिस जज़्बे को रचा गया है, वह महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ लघु फिल्म देखने के लिए लिंक है –
फिल्म में अभिनय किया है – तनुजा कदम, आर्या कुराने, उमेश बोलके, प्रमोद खडतरे, नरेन्द्र देसाई, गिरिजा गोडे, हेमंत धनवाडे, यशवंत चौघले, जयश्री पुरेकर, गार्गी, श्लोका, अन्वी, रसिका, विजय पिश्ते ने।


