अजय आठले
(यह दीर्घ लेख 2011 में लिखा गया है। रायगढ़ इप्टा की वार्षिक पत्रिका ‘रंगकर्म’ के 2011 के अंक में इसी शीर्षक से छपा। अजय के इस लेख को बहुत पसंद किया गया। उसके बाद साथी दिनेश चौधरी ने ‘इप्टानामा’ ब्लॉग में ‘ज्ञानोदय से बाज़ारोदय तक’ शीर्षक से 01 मार्च 2012 के अंक में प्रकाशित किया। संभवतः इसी वर्ष बिलासपुर की महत्वपूर्ण पत्रिका ‘मड़ई’ में भी यह लेख प्रकाशित हुआ। पिछले अंक में पहला भाग पढ़ा, अब प्रस्तुत है दूसरा भाग।)

राष्ट्र-राज्य की कल्पना पूंजीवादी समाज की देन है, लेकिन हमारे देश में यह पूरी तरह से आई ही नहीं। भारत तो एक साथ कबीलाई युग से उत्तर आधुनिक युग में जी रहा है अतः लोक-मनस में राष्ट्र-राज्य की कल्पना कहाँ से आएगी! यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में आज भी बहुत लोग गर्मी की छुट्टियों में ‘देस’ जाना चाहते हैं। लोक-मनस में आज भी राष्ट्र की बजाय देस ज़िंदा है। तभी तो आज भी बिदेसिया लोक-मनस को लुभाता है, फिल्मों में परदेसिया को लेकर कई गाने हिट हो चुके हैं; जबकि वह परदेसिया किसी दूसरे राष्ट्र का न होकर किसी दूसरे गाँव का होता है। आज वैश्वीकरण के इस दौर में जब राष्ट्रवाद भी पिछड़ेपन का प्रतीक हो चुका हो, ऐसी अर्थव्यवस्था का छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

वैश्वीकरण 
राष्ट्रवाद 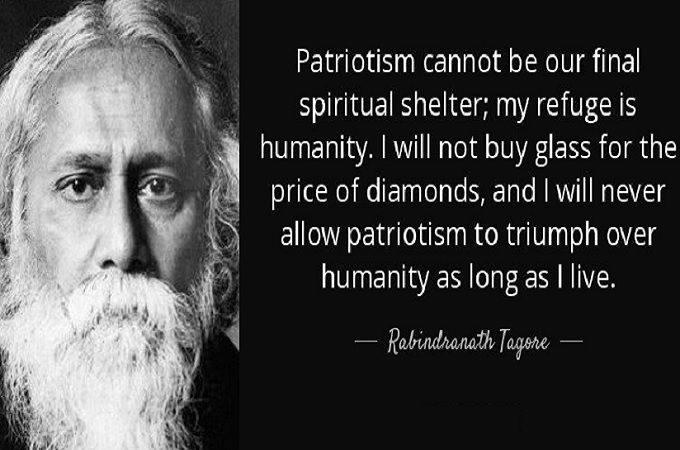
देशभक्ति और मनुष्यता
रायगढ़ के पास ही झारा शिल्पकारों की बस्ती है, जहाँ बेल मैटल का काम किया जाता है। पूर्व में ये अपनी कलाकृतियों में अपने आदिवासी जीवन की झलकियाँ प्रस्तुत करते रहे हैं – कल्पवृक्ष, ताड़ के वृक्ष के नीचे बनी झोंपड़ी में ताड़ी पिलाती आदिवासी महिला आदि। लेकिन आज अपनी कलाकृतियों में ये लोग रामायण और गीता के प्रसंग से लेकर ऐश ट्रे तक बनाने लगे हैं। आदिवासी देवियों को दुर्गा की सात बहनों के रूप में समाहित कर इनका सवर्णीकरण हो गया है और अब यहाँ ज़ोरों से नवरात्रि मनाई जाने लगी है। धर्म का बाज़ार विकसित हो गया है। चन्द्रपुर में बलि प्रथा का विवाद इसी बाज़ार के साथ टकराहट की परिणति था।
सामंतवादी व्यवस्था की विशेषता रही है कि उस काल में धर्म और संस्कृति के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं दिखती लेकिन पूँजीवाद में ज्ञानोदय के साथ ही धर्म और संस्कृति के बीच विभाजक रेखा स्पष्ट हो जाती है लेकिन वैश्वीकरण ने तो धर्म-संस्कृति सबको बाज़ार में समाहित कर लिया। ज्ञानोदय में जो हमने हासिल किया, वह बाज़ारोदय में गँवा दिया।
धर्म का बाज़ार प्रतिरोध की संस्कृति का शमन करने के लिए एक अच्छा हथियार साबित होता है और यह वैश्वीकरण की व्यवस्था के लिए मुफीद भी है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार संस्कृति के नाम पर राजिम कुंभ और संतों के समागम के कार्यक्रम में ज़्यादा व्यस्त है। पूरे देश में बाबाओं का बाज़ार उफान पर है।
संगीत के क्षेत्र में शोर बढ़ता जा रहा है। लय की जगह अब बीट्स ने ले ली है। लोक संगीत के नाम पर, लोकनृत्य के नाम पर भौंडापन परोसा जा रहा है। मनोरंजन उद्योग या कहें बाज़ार उन लोगों के हाथ में है, जिनका छत्तीसगढ़ की लोक परम्परा से कोई वास्ता नहीं है।
लोक संस्कृति को बदलना ही नहीं चाहिए और उसे वैसा ही संरक्षित किया जाना चाहिए, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता और ऐसा संभव भी नहीं है। लोक संस्कृति का जन्म सामूहिक श्रम के कारण हुआ था, सामूहिक रूप से चप्पू चलाते हुए नाविक ‘हैय्या हो हैय्या हो’ गाते थे। अब मोटर बोट को अकेले चलाते हुए नाविक ऐसा कदापि नहीं करेगा।
लोक संस्कृति का स्वाभाविक विकास जनसंस्कृति की ओर होता है। सामंती युग से औद्योगिक युग में पहुँचने पर जनसंस्कृति भी विकसित हुई। व्यवस्था के केन्द्र में जहाँ ईश्वर था, वहाँ मनुष्य केन्द्र में आया परन्तु इस उत्तर औद्योगिक युग में जहाँ वित्तीय पूँजी का बोलबाला है, उसने मनुष्य को केन्द्र से हटाकर बाज़ार को स्थापित कर दिया है और मनुष्य अब मानव संसाधन में बदल गया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया है।
आज की भाषा में कहें तो छत्तीसगढ़ का मानव संसाधन पिछड़ा हुआ है। नई अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियाँ इतनी जटिल हो गई है कि सामान्य जन की समझ से परे है, जो लोग इसे समझ सकते हैं, वे लोग खुद इन्हीं आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। संस्कृति कर्म से उनका वास्ता नहीं है। यही कारण है कि आज इन जटिल परिस्थितियों को लेकर कहानी या नए किस्म के नाटक सामने नहीं आ रहे हैं। पिछले साल रायपुर इप्टा के गजानन माधव मुक्तिबोध नाट्य समारोह में सत्थ्यू साहब के निर्देशन में एक नाटक देखा था, ‘गिरजा के सपने’, जिसमें लोक तत्वों का इस्तेमाल करते हुए बीटी कॉटन के कारण किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का मार्मिक चित्रण था। छत्तीसगढ़ी में हबीब साहब के बाद इस तरह का कार्य नहीं हो रहा है। या तो लोक रूपों को जस का तस पेश किया जा रहा है या फिर हल्की फुल्की कॉमेड़ी पेश की जा रही है। गहरी सोच रखने वाले निर्देशकों की कमी है।

वित्तीय पूँजी वाली अर्थव्यवस्था ने हमारी कार्यशैली को बदल डाला है। शिक्षा के क्षेत्र में अब एमबीए का बोलबोला है। युवा वर्ग स्कूली शिक्षा के बाद सीधे प्रोफेशनल कोर्सेस में जा रहा है, इंजीनियर बनकर एमबीए कर रहा है और बड़ी तनख्वाहों में खप जा रहा है। बेसिक साइंस या सामाजिक विज्ञानों की ओर, उसकी रुचि नहीं रह गई है। हर जगह मैनेज करना सिखाया जा रहा है, चाहे व्यवसाय हो या राजनीति। मैनेजमेंट का मतलब है उपलब्ध संसाधनों से ही परिणाम प्राप्त करना। पहले ‘ऑर्गेनाइज़’ करते थे अब ‘मैनेज’ करते हैं। रंगमंच के क्षेत्र में भी यही हो रहा है। उपलब्ध कलाकारों के हिसाब से नाटक तैयार हो रहे हैं। कलाकारों को नाटक के हिसाब से प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है।
सब कुछ निराशाजनक ही है, ऐसा नहीं है, कुछ प्रगति भी है। इंटरनेट में अब छत्तीसगढ़ के लोगों की दखलंदाज़ी बढ़ी है। वेब पर ब्लॉग भी बढ़े हैं, कुछ अच्छे लेख भी लिखे जा रहे हैं। नई पीढ़ी अब लिखे साहित्य को कम पढ़ती है लेकिन आभासी दुनिया में अपनी दखलंदाज़ी दे रही है। कुछ लघु फिल्में और डाक्यूमेंन्ट्रीज़ भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपलोड की हैं । नई टेक्नोलॉजी अपने स्वरूप में बेहद जनतांत्रिक है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं, यह सुकून देने वाली बात है।

छत्तीसगढ़ में बनी लघु फिल्म 
छत्तीसगढ़ की श्रमजीवी महिलाओं पर डॉक्यूमेंट्री
अभी तो यह संधिकाल है, जहाँ अस्पष्टता बनी हुई है। यह नई अर्थव्यवस्था और पुरानी संस्कृति के टकराव का दौर है। आगे चलकर इनके मिलाप से कुछ नया उपजेगा। हम आशा करते हैं कि ‘‘वो सुबह कभी तो आएगी।’’












बाज़ार ने संस्कृति पर बहुत गहरे प्रभाव डाले हैं। ग्लैमर और भौंडापन को भी संस्कृति का हिस्सा बनाया जा चुका। जो हो “वो सुबह कभी तो आएगी ही “…
बेहतरीन लेख..
इस लेख की एक बात दिल को छू गई. पहले लोग ऑर्गनाइजेड करते थे अब मैनेज करते हैं. 👍 आज के दौर मे मैनेजमेन्ट को सिखाने की जरुरत इतनी पड़ने लगी की शिक्षा ने भी हाथ सेकने शुरू कर दिए. हाय रे! संकुचित तेरा क्या करें
एमबीए ने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। ना तो एमबीए पढ़ा है और ना ही इसका सिलेबस देखा है। पर इसका प्रभाव देखता हूं, कि कैसे भी उत्पादन लागत को कम किया जाए और स्कीम बनाकर अधिक मात्रा में बेचा जाए। प्रॉफिट, जीडीपी सब बढ़ा लेना चाहते हैं। नतीजा, पृथ्वी थर थरा गई है। सारे संसाधनों को चूस लेना चाहते हैं। जैसे, गाय को इंजेक्शन लगाकर, बिना ब्रेक के, लगातार दूध प्रोडक्शन करवाना बिजनेस है। जनता के
स्वास्थ्य से कोई लेना देना है?
मानसिक अशांति से 35 साल के सीईओ आत्महत्या कर रहे हैं या हार्ट अटैक से जान गंवा रहे हैं।
क्यों पिछले साल से ज्यादा रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी बिकना चाहिए? क्यों और अधिक मकान बनाए जाने चाहिए, जो कंक्रीट जंगल बनता है और एसी चलाकर ही रहने लायक होता है?
मुड़ कर देखें तो वह धीमा सुविधा रहित जीवन बड़ा ही सुगम, प्राकृतिक लगता है