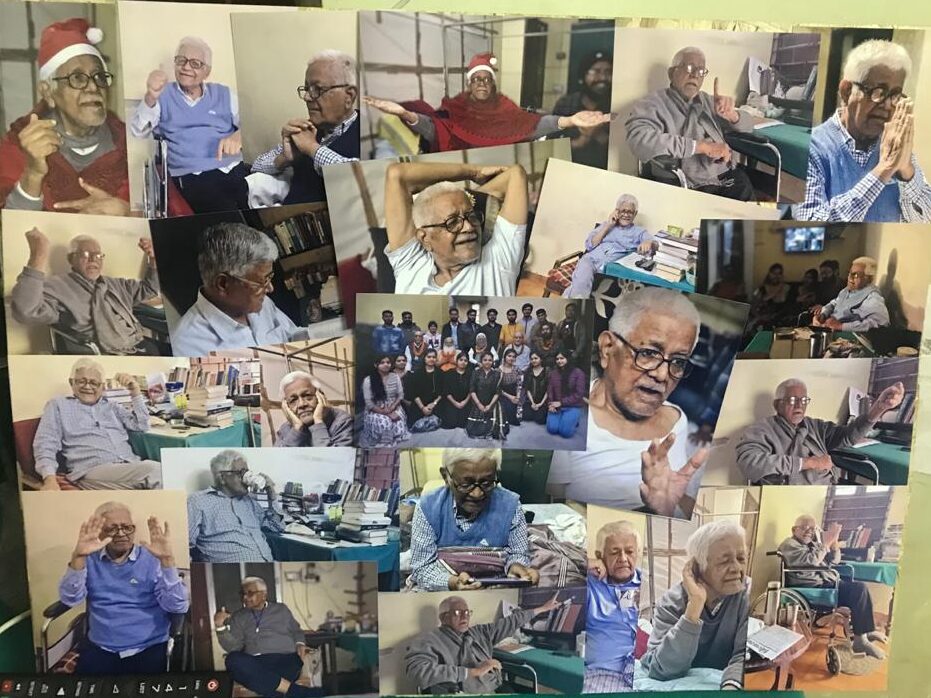(प्रगतिशील लेखक संघ, बिलासपुर ने 7-8 नवम्बर 2009 को महत्व राजेश्वर सक्सेना नामक आयोजन किया था। यह लेख उस आयोजन में पढ़ा गया तथा राजेश्वर सक्सेना जी के कार्यों पर प्रकाशित पुस्तिका का हिस्सा भी बना। सर ने लगभग 1980 से लेकर आज तक सैकड़ों लोगों को जो वैचारिक प्रकाश और ऊर्जा से आप्लावित किया है और आज भी ख़राब स्वास्थ्य के बावजूद वे युवाओं के मार्गदर्शक बने हुए हैं, उसके लिए उन्हें लाखों-लाख सलाम!!! मेरी ज़िंदगी को सार्थक दिशा देने का सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हें ही है। यहाँ तक कि रायगढ़ इप्टा के साथी अजय आठले से मेरी शादी की पहल करने से लेकर हमारे वैवाहिक जीवन और सांगठनिक सक्रियता के प्रति भी उनका बहुत आत्मीय नज़रिया रहा है। वे हमें देखकर बहुत खुश होते थे। हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रति वे हमेशा बहुत उत्सुक बने रहे। अजय के विचारों की नवीनता उन्हें हमेशा आकर्षित करती थी। – उषा वैरागकर आठले)
कक्षा में सर काव्यशास्त्र और मुक्तिबोध पढ़ाते थे, परंतु छोटे-छोटे विषय देकर वे हमें लेख लिखने के लिए कहते। मेरी भाषा पर मराठी के प्रभाव ओर होने वाली गलतियों को हमेशा रेखांकित करते। उन्होंने बात-बात में जान लिया था कि मैं कविताएँ लिखती हूँ। अचानक एक दिन उन्होंने मुझे अपनी कविताओं के साथ प्रगतिशील लेखक संघ की कवि गोष्ठी में आमंत्रित किया। मैं जब वहाँ पहुँची, वहाँ नवल शर्मा, प्रताप ठाकुर, रफीक खान, मंगला देवरस, प्रभा खरे आदि मौजूद थे। अपने से काफी बड़े और अध्ययनशील लोगों के बीच पहुँचकर मैं थोड़ा घबराई थी। सर के कहने पर मैंने अपनी बहुत ही कच्ची कविता का संकोच के साथ पाठ किया था। अन्य लोगों की कविताएँ भी सुनी थीं। लगातार कविताएँ लिखते रहने के लिए सभी ने प्रोत्साहन दिया। उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ की प्रत्येक गोष्ठी में सर मुझे आमंत्रित करते। सर शायद मुझमें संभावनाएँ टटोल रहे थे। उन्होंने मुझे घर बुलाना शुरु किया। हर बार जाते ही एक या दो किताबें थमा देते। उसमें से किसी विशेष अध्याय को पढ़ने के लिए कहते या पूरी किताब। मैं पढ़ने की कोशिश करती, मगर अधिकांश चीज़ें मेरे सर पर से निकल जातीं। मुसीबत यह थी कि बिना पढ़े उनके घर नहीं जा सकती थी क्योंकि जाते ही सवाल दागा जाता – ‘‘कितने पन्ने पढ़े? क्या समझ में आया?’’ बिना पढ़े क्या जवाब दूँ! इसी शर्म और लिहाज़ के कारण जब तक किताब नहीं पढ़ लेती थी, तब तक उनके घर नहीं जा पाती थी। हालाँकि धीरे-धीरे सर ने पढ़ने की और समझने की आदत डाल ही दी। जो समझ में नहीं आता था, उसे पूछने की वे पूरी छूट देते थे। इतना श्रम, समय, पुस्तकें और आत्मीयता उस समय भी कोई प्राध्यापक नहीं देता था।
सर के घर का सबसे बड़ा आकर्षण था, उनके घर रोज़ होने वाली वैचारिक जंग वाली बैठकें। अक्सर आठ-दस साथी शाम को छै-साढ़े छै बजते ही आ जाते। ताज़ा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर संगठन, विचारधारा, फिल्म, कला, विभिन्न नई किताबों और पत्रिकाओं पर बातचीत चलती। कभी-कभी बहुत गर्मागर्म बहस भी छिड़ जाती, परंतु दूसरे दिन सब सामान्य हो जाता और विचारों को साझा करने का सिलसिला फिर चल पड़ता। पहले ये बातें भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती थीं। सर ने एक दिन पूछा – ‘‘कौनसा अखबार पढ़ती हो? घर में कौनसा अखबार आता है? रोज़ पढ़ा करो।’’ सर के घर पर होने वाली बातें भले ही मेरी समझ में न आती हों, परंतु शुरु से उनके प्रति एक अदम्य आकर्षण महसूस होता था। अखबार और अन्य पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ते-पढ़ते कब वे बातें समझ में आने लगीं और कब मैं भी उनमें भाग लेने लगी, पता ही न चला।

सर के ही निर्देशन में पीएच.डी. के लिए आवेदन देने के बाद उन्होंने किताबें खरीदने की आदत डाली। न केवल हिंदी साहित्य, बल्कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मानवशास्त्र, अंग्रेज़ी साहित्य, रूसी साहित्य की महत्वपूर्ण किताबें खरीदवाईं। पीएच.डी. के लिए किये जाने वाले शोध कार्य के अध्ययन का दायरा इतना विस्तृत बना दिया था कि अधिक से अधिक जानने का एक जुनून सवार हो गया। ‘जनसत्ता’, ‘मेनस्ट्रीम’ जैसे अखबार पढ़ने का चस्का लगाया। इसी बीच सर ने मार्क्स-एंगेल्स की संकलित रचनाओं के वॉल्यूम देना शुरु किया। पढ़ने का एक सिलसिला चल पड़ा, ड्यूहरिंग मत खंडन, मार्क्स के भारत विषयक लेख, मार्क्स और लेनिन की जीवनी, गोर्की का प्रसिद्ध उपन्यास ‘माँ’, निकोलाई आस्त्रोव्स्की का ‘अग्निदीक्षा’, हावर्ड फास्ट का ‘समरगाथा’… … एक अंतहीन विचार और क्रियाशीलता को उत्प्रेरित करने वाली साहित्य-यात्रा पर मैं चल पड़ी थी सर की उंगली थामे हुए। मेरे अन्य साथी भी थे। हम सब खूब पढ़ते, चर्चा करते। सर से भी बहस करते। सर के असीमित ज्ञान से डरते ज़रूर थे पर कुछ भी पूछने में झिझकते नहीं थे। अपनी तमाम शंकाएँ, संदेह सर के सामने समाधान की उम्मीद में रख देते थे। हरेक रचना पढ़कर उसका विश्लेषण करने का अभ्यास, अपना मत प्रकट करने का साहस धीरे-धीरे विकसित होता चला गया। मुझमें आत्मविश्वास बढ़ रहा था। शाकिर भाई, मधुकर, प्रताप, रफीक, अरूण, हबीब भाई, गंगाप्रसाद ठाकुर जैसे साथियों के बीच मैं प्रायः अकेली लड़की होने के कारण सर मुझे लेकर बहुत चिंतित भी रहते थे। वे प्रायः गीता मौसी को भी मेरे साथ बैठा देते थे। उनके व्यक्तित्व के इस पहलू से मैं उस वक्त काफी परेशान रहती थी, मुझे इसमें उनका अविश्वास नज़र आता था, मगर इस पितृवत स्नेह का अहसास मुझे उम्र के अगले पड़ावों में महसूस हो पाया।

मुझे दार्शनिक साहित्य की अपेक्षा सरल सैद्धांतिक-व्यावहारिक या सृजनात्मक साहित्य पसंद था। ‘कम्युनिस्ट नैतिकता’, ‘हम अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बने’ जैसी किताबें पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद था अपेक्षाकृत ‘ड्यूहरिंग मत खंडन’ के। परंतु सर हमारी वैचारिक नींव पक्की करने के लिए कोई न कोई बात छेड़ देते, हमारी जिज्ञासा बढ़ा देते और फिर कोई किताब थमा देते। उसके बाद उस किताब पर बातचीत का लम्बा सिलसिला बन जाता।
उन दिनों प्रगतिशील लेखक संघ की बिलासपुर इकाई हम युवा साथियों के उत्साह और सक्रियता से सुर्खियों में थी। सन् 82-83 में हम जबलपुर में आयोजित ‘महत्व शमशेर’, जगदलपुर में आयोजित चौथे राज्य सम्मेलन और जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में 10-12 साथियों का दल लेकर गए। यात्रा में आते-जाते रास्ते भर सिर्फ चर्चा, चर्चा और चर्चा चलती थी। आयोजन स्थल पर प्रायः पुस्तक-प्रदर्शनी लगती थी। हम खूब किताबें खरीदते। सर की सलाह सर्वोपरि होती थी। वहाँ आए हुए पूरे देश भर के रचनाकार साथियों से मिलते, सबको सुनते और बातें करते। खट्टे-मीठे अनुभवों के बीच वैचारिक समृद्धि का वह दौर, एक बहुत वृहद संगठन से जुड़े होने का गर्वभरा अहसास और प्रतिबद्धता के आदर्श से लबालब भरे हमारे हृदय सुकून से भरे हुए थे। सर को एक मामूली रकम पकड़ाकर हम कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मुक्त हो जाते। सर ही टिकट, खानपान, आवास, रिक्शा भाड़ा आदि की व्यवस्था देखते और हम उनके पालकत्व की छाँव में निश्चिंत होकर संगठन की दुनिया में डूबते-उतराते।

प्रगतिशील लेखक संघ में सक्रिय होकर मुझे दो साल भी नहीं हुए थे कि सर ने एक दिन बताया कि ‘‘बिलासपुर में इप्टा की इकाई शुरु करनी है। तुम तो मराठी नाटक करती ही हो, अब इप्टा के साथ हिंदी नाटक करना।’’ मैंने स्कूल तक हिंदी नाटकों में अभिनय किया था परंतु मैं पूरीतरह मराठी नाटकों का ‘प्रोडक्ट’ थी। (चूँकि मेरे आई-बाबा मराठी शौकिया रंगमंच में लगातार सक्रिय थे) फिर भी सर को मना करने की हिम्मत नहीं हुई। सर के घर की छत पर रायपुर इप्टा के साथी राजकमल नायक के निर्देशन में प्रति शनिवार-रविवार को वर्कशॉप शुरु हुआ। थियेटर एक्सरसाइज़ेस से शुरु कर उन्होंने भारतेन्दु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध प्रहसन ‘अंधेर नगरी’ खड़ा किया। रेल्वे इंस्टीट्यूट में उसका प्रथम मंचन हुआ। उसके बाद अन्य गाँवों में और रायपुर में भी मंचन हुए। मेरे सामने हिंदी थियेटर की एक नई दुनिया खुल गई, जो अब तक किये मराठी नाटकों की दुनिया से एकदम अलग थी। यहाँ नाटक के विषय, प्रस्तुति शिल्प और उद्देश्य भी सामाजिक सरोकार से जुड़े होते। सर नाटक की रिहर्सल से लेकर उसके मंचन तक की सारी व्यवस्था प्रगतिशील लेखक संघ के अन्य साथियों के साथ करते थे। समूचा अर्थ-प्रबंधन और व्यवस्था-प्रबंधन उनके निर्देशन में ही चलता। हम सब अपनी-अपनी साइकिलों पर सवार होकर टिकट बेचने जाते। नाटक के लिए लड़कियों को तैयार करते। कास्ट्यूम का जुगाड़ करते। सारी तैयारियों में सर हमारे साथ होते – पूरी ऊर्जा, ताकत और उत्साह से भरपूर। अपनी दमे की बीमारी को वे तब ठेंगा दिखाते थे।
सर ने जिसतरह अपने व्यवहार और मार्गदर्शन से मुझे दोनों संगठनों का एक प्रतिबद्ध, कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता बनाया, उसीतरह उन्होंने मेरे लेखन पर भी पूरा ध्यान दिया। न केवल अकादमिक रूप से उन्होंने मेरी नींव मजबूत की, बल्कि ज्ञानरंजन जी द्वारा मराठी से हिंदी अनुवाद के लिए प्रस्ताव दिये जाने पर मुझे इस दिशा में भी प्रेरित किया। आज भी मैं जो अनुवाद का काम हाथ में लेती हूँ, सर उसमें पूरी दिलचस्पी लेकर काम की प्रगति का जायज़ा अवश्य लेते हैं। मेरे विद्यार्थियों को भी वे उसीतरह मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसा अपने विद्यार्थियों को देते थे।

एक अन्य बात का उल्लेख किये बिना बात पूरी नहीं हो सकती। सर के लेखन से भी मुझे सिद्धांतों की गहराई तक पैठने और विश्लेषण करने का प्रशिक्षण मिला। उन दिनों सर के अनेक लेख और किताबें पहली बार मुझे ही पढ़ने का सौभाग्य मिलता था क्योंकि मेरी लिखावट स्पष्ट और अच्छी होने के कारण सर टाइपिंग के लिए देने से पहले मुझे अपने सामग्री का अंतिम प्रारूप लिखने के लिए देते थे। इस पुनर्लेखन ने मुझे सर के विचार-सूत्रों को समझने में काफी मदद दी थी। सामान्यतः बहुत सी बातें किताब एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आती थीं, परंतु जब उनका पुनर्लेखन किया जाता था तो दो-तीन बार पढ़ने की प्रक्रिया में वे सूत्र काफी कुछ स्पष्ट हो जाते थे। अंतिम प्रारूप उन्हें सौंपते हुए मैं उनसे वे भी बिंदु स्पष्ट कर लेती थी, जो मुझे समझ में नहीं आते थे।
आज मैं रायगढ़ में रहते हुए इस चीज़ की बहुत कमी महसूस करती हूँ। पहले भी सर का विचार-दर्शन शत-प्रतिशत ग्रहण नहीं कर पाती थी, पर अब तो लगता है कि मैं बहुत पीछे छूट गई हूँ और सर विचारों की दुनिया में मीलों आगे निकल गए हैं। मैं अपनी घर-गृहस्थी, अध्ययन-अध्यापन, अनुवाद, नाटक, सामाजिक कार्यों की दुनिया में खोकर काफी पिछड़ गई हूँ। कक्षा में पहले दिन हाथ में पकड़ा हुआ ज्ञानात्मक संवेदना का सिरा आज भी मेरे हाथ में है परंतु सर की वैचारिक पतंग बहुत दूर आसमान में उड़ रही है, जिसे सिर्फ निहारा ही जा सकता है।
मैं, प्रताप और रफीक जब भी मिलते हैं, गर्व से कहते हैं, हम ‘सक्सेना स्कूल’ के छात्र हैं। सक्सेना स्कूल का अर्थ ही है – ईमानदारी और सामूहिकता में की जाने वाली जी-तोड़ मेहनत, भरपूर और गहरा अध्ययन-मनन-चिंतन, विचार-विमर्श और लेखन। मैं अपनी ओर से सर को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि उनके द्वारा रोपे गए ये मूल्यवान संस्कार मेरे भीतर हमेशा ज़िंदा रहेंगे, मुझे हमेशा सक्रिय रखेंगे।